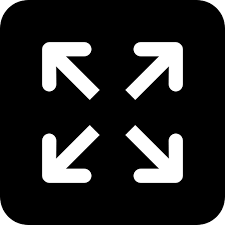कंडोम, समलैंगिकता और जाति से आविष्ट कविता

अष्टभुजा शुक्ल की कविताएं पढ़ रहा हूं। उनकी एक कविता है ‘हलन्त’।
इसमें शुक्ल कहते हैं:
हलन्त ने “कभी दावा नहीं किया
कि देवनागरी के स्थापित वर्णों के संसार में
आरक्षित हो उसकी जगह”
हलंत हमारी लिपि में प्रयुक्त होने वाला बहुत पुराना चिन्ह है, जो संस्कृत में भी इस्तेमाल होता है। उपरोक्त कविता में हमारा ध्यान 'देवनागरी' शब्द की ओर जाना चाहिए। 'देवनागरी' क्यों? सिर्फ 'नागरी' क्यों नहीं? क्या इसमें ‘देव’ लगाकर इसे एक खास तबके द्वारा विकसित लिपि होने का परोक्ष रूप से दावा नहीं ठोका जा रहा है?
जबकि प्रमाण इसके उलट हैं। लिपियों का निर्माण शूद्रों ने किया, ब्राह्मण इस काम में सक्षम नहीं थे।
पुरातात्त्विक प्रमाण बताते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी है। ये लिपियां अशोक के शिलालेखों की लिपि हैं। नागरी लिपि इसी ब्राह्मी लिपि से निकली है। केवल संस्कृत ग्रन्थों में ही इसे 'ब्राह्मी', यानी ब्रह्मा से उत्पन्न कहा गया है।
जैन-बौद्धों के पालि-अपभ्रंश ग्रन्थों में इसे ‘बम्भी’ और अशोक के शिलालेखों में इसे ‘धम्म लिपि’ कहा गया है। वस्तुतः इसका मूल नाम 'बम्भी' और 'धम्म' लिपि ही है।
नागरी के साथ जिस उद्देश्य से 'देव' लगाया जाने लगा, उसी उद्देश्य से 'बम्भी' और 'धम्म' को 'ब्राह्मी' कहा गया। यह सब भाषा पर आधारित सामाजिक श्रेणीकरण बनाने के तरीके हैं।
जाहिर है, इस मामले में अष्टभुजा शुक्ल अकेले नहीं हैं। अन्य लोग भी जाने-अनजाने ऐसे प्रयोग करते रहते हैं।
भारत ही नहीं, दुनिया की किसी भी सभ्यता में लिपियों का आविष्कार विद्वानों ने नहीं, चित्रकार और मूर्तिकारों ने किया। भारतीय उपमहाद्वीप में ये मूर्तिकार और चित्रकार कौन थे? हिंदू शास्त्रों ने इन्हें शूद्र कहा है। जितने भी कामगार हैं, भारत उन्हें शूद्र श्रेणी में रखा गया है। लोक प्रचलित नृत्य, गीत, भाव और भंगिमाओं के आधार पर उन्होंने चित्र और मूर्तियों को उकेरा। लिपियों के अतिरिक्त लोकभाषा और लोकगीत इन्हीं कामगार वर्गों के घर-परिवार और समाज से निकले। ('हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में दलित-पिछड़ों का योगदान', हरिनारायण ठाकुर)
बहरहाल, लिपि को शूद्र-ब्राह्मण-द्विज में विभाजित करके देखना उचित नहीं है। वह हम सबकी है। भाषा की तुलना में लिपियों में परिर्वतन बहुत धीमा और बहुत कम होता है। इसका निर्माण भले ही शूद्रों ने किया हो, लेकिन इतने लंबे कालखंड में, इसके विकास के विभिन्न चरणों में इसे बरतने वाले सभी समुदायों ने इसे अपनी मेधा और कल्पनाशीलता से संवारा और संजोया है। हम इस लिपि से चंद्रबिंदु गायब कर इसे सरल बनाने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को भी कैसे भूल सकते हैं? इसी प्रकार उन प्रकाशकों को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने इसके पूर्ण विराम की डंडी को रोमन के बिंदु वाले फुल स्टॉप में बदलकर इसका सौंदर्य बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब परिवर्तन सार्थक हैं और हमारी लिपि को बदले हुए समय और तकनीक के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
हम अपने मूल विषय की ओर लौटें तथा अष्टभुजा शुक्ल की उपरोक्त कविता की कुछ और पंक्तियां देखें:
“वर्णों की जैविकी में
एककोशीय अमीबा की तरह
यह गोंजर की जली हुई टांग की तरह
या विकलांग वर्णों की
वैसाखी की तरह
(हलंत को)
बस किसी शब्द की
हुंकारी चाहिए उसे अथवा अपनापा”
फिलहाल यह छोड़ दें कि “विकलांग वर्ण” और क्या ध्वनित हो रहा है। ‘गोंजर’ शब्द पर ध्यान दें। उन्होंने कनगोजर या कनखजूरा नहीं लिखा। मूल शब्द गोंजर का पकड़ा, जो ठीक भी है और बताता है कि अष्टभुजा जी शब्दों के प्रयोग को लेकर कितने सर्तक हैं। इतना सर्तक नागरी के प्रति क्यों नहीं रह सके?
इधर दो राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड को देवभूमि कहने का चलन बढ़ा है। यह देव भूमि, देव नगरी क्यों? मनुष्यों की भूमि और मनुष्यों की नगरी है, उसे उसके अपने नाम के साथ ही जीने दो न।
बहरहाल, अष्टभुजा शुक्ल की अनेक कविताओं का कथ्य भी बहुत समस्याग्रस्त है। उनमें प्रतिक्रियावादी मूल्य भरे पड़े हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए लगता है कि वे समाज को पीछे ले जाने वाले कवि हैं।
उनकी एक कविता है “भारत घोडे़ पर सवार है”, जिसे जनवादी युवा मनोयोग से गाते हैं। इप्टा आदि के कार्यक्रमों में भी यह लोकप्रिय कविता खूब चलती है।
इस की कुछ पंक्तियां देखिए:
“एक हाथ में पेप्सी कोला
दूजे में कंडोम
तीजे में रमपुरिया चाकू
चौथे में हरिओम”
शुक्ल कंडोम को नकारात्मक अर्थ में रखते हैं। वे कौन से मूल्य हैं, जो उन्हें इसके लिए प्रेरित करते हैं? क्या वे वही कथित लोकमंगलवादी मूल्य नहीं हैं, जिसके लिए स्त्री और शूद्रों की आजादी एक बड़ा खतरा है।
यह कंडोम ही है जिसने स्त्री-आजादी को नई उड़ान दी। यह विश्व के सामाजिक इतिहास को प्रगतिशील दिशा देने वाला साबित हुआ है तथा इसने सिर्फ स्त्रियों को ही नहीं, पूरी मनुष्यता को आजाद बनाने में भूमिका निभाई है। इसका आना एक मूक क्रांति था, जिसने दुनिया को बदलने में मार्क्सवाद के बराबर भूमिका निभाई है। एक विचार के रूप में मार्क्सवाद को एक न एक दिन पुराना पड़ना ही था। मार्क्सवाद का नाता हमारे विचारों से, हमारे जीवन के बाहरी तत्व से था। लेकिन गर्भनिरोधक उपायों के आने से जो क्रांति हुई है, उसने मानव जाति को जैविक स्तर पर प्रभावित किया है। इस क्रांति का असर तब तक रहेगा, जबतक मनुष्य जाति अपने इस रूप में है।
खैर, जैसा कि मैंने पहले कहा, शुक्ल जी का कंडोम से बिदकना और उसे अश्लीलता की श्रेणी में रखना यूं ही नहीं है। दरअसल, वे ‘पेप्सी कोला, 'कंडोम' और 'रामपुरिया चाकू' जैसी गलत चीजों के बरख्श ‘हरिओम’ को रखते हैं। वे चेतन-अचेतन रूप से ‘हरिओम’ को समाज का तारक मानते हैं।
यह अनायास नहीं है कि तुलसी उनके प्रिय कवि हैं और रामचरित मानस उनका प्रिय ग्रंथ है। ऐसा उन्होंने अनेक जगहों पर कहा है।
बहरहाल, इसी कविता में आगे है:
“एड्स और समलैंगिकता की
रहे सलामत जोड़ी
विश्वग्राम की समता में
हमने सीमाएं तोड़ी
दुनिया पर एकाधिकार है
भारत घोड़े पर सवार है”
आप इसमें देखें कि वे सेक्सुअलिटी को कैसे देख रहे हैं, कहां खड़े होकर देखकर रहे हैं? इसमें सिर्फ बाजार का अंध विरोध ही नहीं है, बल्कि इस विचार के पीछे मनुष्य की निजी आजादी का विरोध और ऐसा शुचितवाद है, जो कभी धर्म तो कभी बाजार के विरोध के नाम पर सामाजिक यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है।
कवि की नजर में समलैंगिकता एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा दुर्गुण है जो उदारीकरण और बाजार के कारण हमारे देश में आया है। ये बीमार लोग हमारे पवित्र समाज और धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। पता नहीं वे इस बीमारी को ठीक करने का क्या उपाय देखते हैं?
वे इसी कविता में आगे 'आर्यपुत्र' को याद करते हैं, जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि वे विदेशियों और द्रविड़पुत्रों से इस देश को बचाने में सक्षम हैं।
"दुनियावालों आकर देखो
यहां अहिंसा रोती
जाती हुई सदी में भारत
खोल चुका है धोती
आर्यपुत्र को रथ विकार है।"
इन कविता-पंक्तियों से बहती वैचारिक प्रतिगामिता इतनी स्पष्ट है कि उसे व्यंग्य-रचना की आड़ में नहीं छुपाया नहीं जा सकता।
कुछ अन्य पंक्तियां इस प्रकार हैं:
"आठ हजार जेन की मारूती
बिकी मुक्त बाजार
एक हजार पुस्तकें छप कर
पड़ रहीं बेकार
वैभव द्विज, रचना चमार है"
यह कैसी उपमा है? कवि का मन जाति में इतना गहरे क्यों धंसा है कि उसे यह ध्यान नहीं आता कि वह एक श्रमशील कौम की सामाजिक रूप से निम्न स्थिति पर अपनी मुहर लगा रहा है? क्या चमार द्विज से हीन हैं? किसी सुबुद्ध कवि को त्याज्य सामाजिक मान्यताओं को क्यों अपनी कविता में दुहराना चाहिए?
जैसा कि मैंने पहले बताया अष्टभुजा शुक्ल की यह कविता वाम संगठनों में इतनी लोकप्रिय है कि कार्यक्रमों में इसे सामूहिक रूप से गाया जाता रहा है। अगर आपको महसूस करना हो कि उपरोक्त पंक्तियां कितनी दाहक हैं तो कल्पना करें कि आप चमार जाति में पैदा हुए हैं और ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आपको उपरोक्त पंक्तियों का सार्वजनिक पाठ करना है।
हिंदी साहित्य की कथित मुख्यधारा का एक अच्छा-खासा हिस्सा ऐसी ही यथास्थितिवादी और प्रगतिगामी चीजों से निर्मित है। इसलिए मेरी इस टिप्पणी को इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि अष्टभुजा जी पर कोई हमला कर रहा हूं। उनकी हलन्त शीर्षक कविता पढ़ते हुए ये बातें याद आईं तो लगा कि लिख देना बुरा नहीं होगा।
हमारे समाज के साथ-साथ साहित्य और विमर्श की दुनिया में भी लंबे समय से विचारहीनता पसरी हुई है। हिंदी साहित्य में पिछले साठ साल से सबकुछ ‘समकालीन’ है। कोई नई चीज, कोई नई जरूरत हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जबकि इस बीच दुनिया कहां से कहां निकल चुकी है। इसलिए मेरे जैसे लोग कहते हैं कि बहुजन साहित्य की अवधारणा को आने के लिए जगह दें। उस से सूरत बदलेगी।
[प्रमोद रंजन की दिलचस्पी सबाल्टर्न अध्ययन और तकनीक के समाजशास्त्र में है। संप्रति, असम विश्वविद्यालय के रवीन्द्रनाथ टैगोर स्कूल ऑफ़ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज़ में सहायक प्रोफ़ेसर।]