
अंकल सैम दूर के..., आप खाएं थाली में, भारत को दें प्याली में!
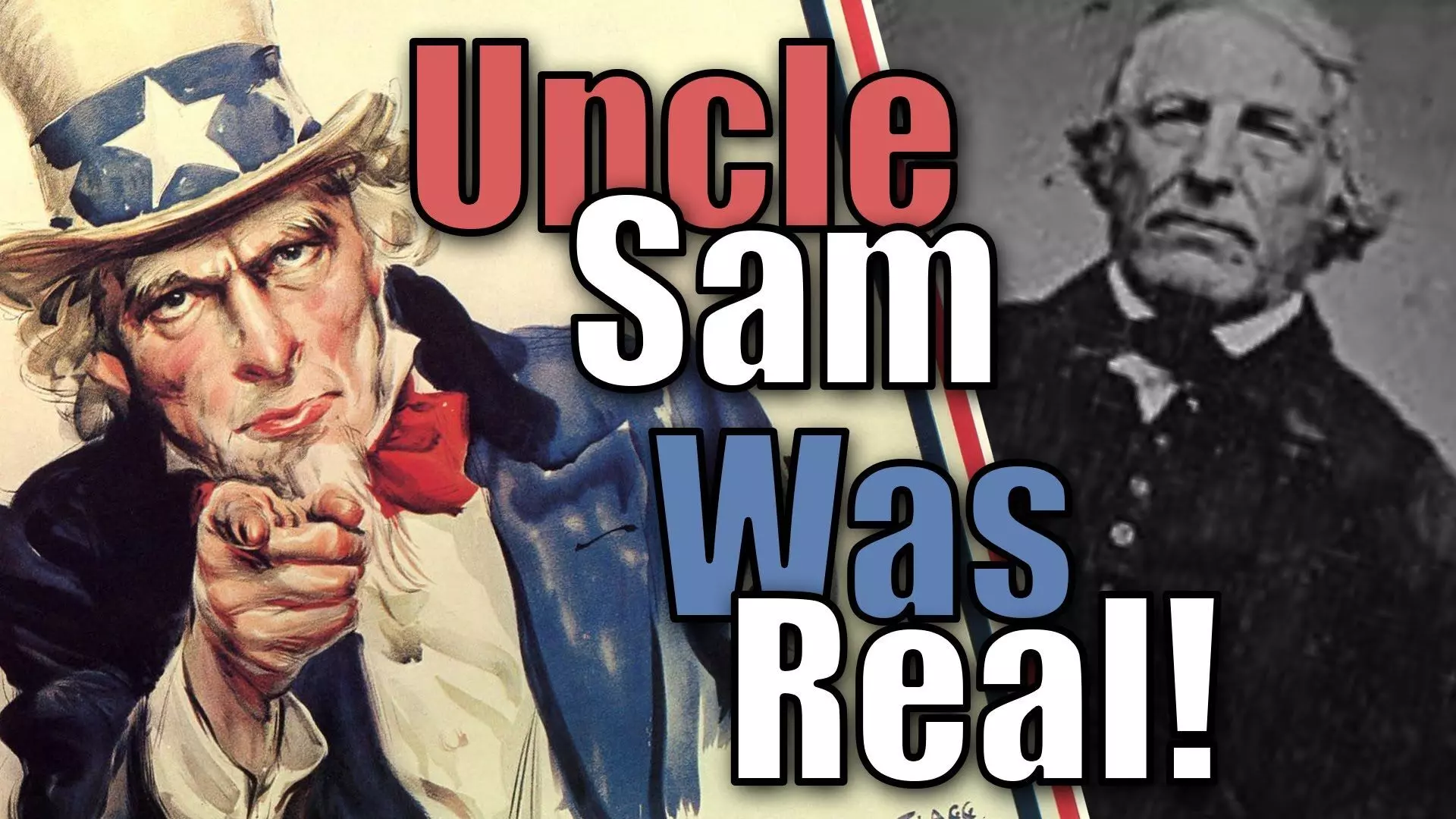
खरगोशों की तरह भारतीयों को भी खाना खिलाना और उसके लिए हमारे द्वारा रोजाना 10 लाख का खर्च उठाना, कुछ ऐसा ही है, जैसे हम विश्वयुध्द के दौरान हाथ पर हाथ धर कर बैठे हों।
- (1942 में अकाल पीड़ित बंगाल को अनाज भेजे जाने पर आपत्ति जताते हुए कैबिनेट बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का कथन)
भारत जैसे तमाम देशों में बढ़ती समृध्दि एक तरह से अच्छी तो है मगर बेहतर पोषण की इनकी बढ़ती मांग ही है, जिसके कारण दुनियाभर में आज खाद्यान्न की कीमतों में आग लगी हुई है।
- (मई 2008 में हुए एक सम्मेलन के दौरान वैश्विक खाद्यान्न संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डबल्यू. बुश का भारत जैसे उभरते देशों पर दोषारोपण)
1942 से लेकर 2008 के बीच बहुत कुछ बदल गया। नहीं बदला तो दुनिया के इन 'हुक्मरानों' का वह शाही अंदाज, जिसके तहत वे अपने राज-पाट की किसी भी बदहाली का जिम्मेदार भारत को ही मानते रहे।
चर्चिल के इस दंभभरे बयान के चंद बरसों के भीतर ही भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से ब्रिटिश पताका तो उखड़ गई लेकिन धीरे-धीरे शक्ति संतुलन अमेरिका के पक्ष में आ गया। और भले ही उस दौर के ब्रिटिश राज जैसा साम्राज्य आज अमेरिका का नहीं हो, लेकिन कमोबेश उसी रौब-दाब के साथ वह पूरी दुनिया पर परोक्ष-अपरोक्ष तौर पर काबिज है।
शायद इसीलिए इस आधुनिक 'विश्वविजेता' में भी वही ब्रिटिश दंभ नजर आ रहा है, जिसके तहत खुद के पास तो छत्तीस भोग की थाली होनी चाहिए लेकिन 'मदारी, सपेरों, साधु और भिखारियों' के देश भारत की उसकी 'प्रजा' को बामुश्किल दो-जूल की दाल रोटी ही मयस्सर होनी चाहिए।
लेकिन इस दंभ में वह यह भी न जाने क्यों भूल गया कि भारत अब न तो किसी का गुलाम है, और न ही 'मदारी, सपेरों, साधु और भिखारियों' का देश..., भारत तो अब हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर और परमाणु-आर्थिक-तकनीकी-अंतरिक्ष जैसे तमाम अहम क्षेत्रों में महाशक्ति बनने की कगार पर खड़ा है। खुद अमेरिकी और यूरोपीय देशों का बाजार इसके सामने नतमस्तक हो चुके हैं।
भारतीय बाजार की समृध्दि का आलम यह है कि भारतीय कंपनियां, धनकुबेर और भारतीय प्रतिभाएं अमेरिका समेत पूरी दुनिया को धीरे-धीरे अपनी मुट्ठी में जकड़ते जा रहे हैं। जाहिर है, अब समृध्दि बढ़ेगी तो भारतीयों को अच्छा खाने का मन करेगा।
और यह भी सच है कि इतनी बड़ी आबादी अगर चंद बरसों के भीतर ही अच्छी खुराक खाने लगेगी तो वैश्विक तौर पर खाद्यान्न बाजार के समीकरण उलट-पुल होंगे। लेकिन इसका यह मतलब तो कतई नहीं होना चाहिए कि एक बार फिर उसकी थाली से ये पकवान छीनकर उसे वापस गरीबी और भुखमरी के अंधेरों में ढकेल दिया जाए।
अगर दशकों से पूरी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी और यूरोपीय लोगों का दबदबा रहा है तो अब भारत और चीन जैसे एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों के लोगों को भी उनका हक तो लेने दीजिए।
इससे बाजार के समीकरण अगर गड़बड़ा रहे हैं तो उसे सही करने के और भी रास्ते हैं। मसलन, उत्पादन को बढाया जाए, सही वितरण प्रणाली को अपनाया जाए या फिर विकास और अपनी जरूरत के नाम पर बायोफ्यूल जैसे खाद्यान्न उत्पादन के जानी-दुश्मन कदमों पर या तो नियंत्रण किया जाए या फिर उनसे तौबा की जाए। लब्बो-लुवाब यही है कि बजाय एक-दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के, इस समस्या को बदलते समय के परिप्रेक्ष्य और हालात के आइने में रखकर मिल-जुलकर सुलझाया जाए।
ऐसा नहीं है कि जनाब बुश या अमेरिका ही दुनियाभर में हो रहे खाद्यान्न संकट को लेकर घबराए हुए हैं बल्कि इसकी चिंता खुद भारत और चीन जैसे उन तमाम देशों को भी है, जिनपर इसके लिए दोषारोपण किया जा रहा है। खाद्यान्न की बढ़ती कीमतें, उनकी कमी और उत्पादन, ये ऐसी समस्याएं हैं, जिनसे इन दिनों खुद भारत को भी बड़े पैमाने पर दो-चार होना पड़ रहा है।
यह भी एक वजह है कि ऐसे मुश्किल समय में भारत पर ही उंगली उठाने वाले बुश के बयान से यहां हर गली-कूचे में हंगामा खड़ा हो गया। बहरहाल, इसी हंगामे के मद्देनजर बुश के आरोप के हर पहलू को समझने और पाठकों-विशेषज्ञों की राय से रूबरू होने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ने व्यापार गोष्ठी में इसी मसले को लिया। देशभर से आ रहे बेशुमार पत्रों ने यह साबित भी कर दिया कि यह मसला वाकई किस कदर लोगों के लिए अहम है।
क्षमाप्रार्थना के साथ सुधी पाठकों से हम यह भी कहना चाहते हैं कि स्थानाभाव की गंभीर दिक्कत के कारण अगर इस बार हम उनके पत्र को इस विशेष पृष्ठ में जगह न भी दे पाए तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसे आने वाले दिनों में यथाशीघ्र संपादकीय पृष्ठ के पक्ष-प्रतिपक्ष कॉलम में जगह अवश्य दें।
यह खबर अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने May 12, 2008 को लिखी थी.




