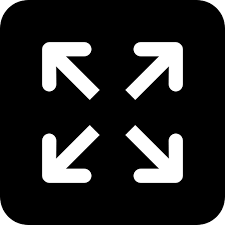- Home
- /
- हमसे जुड़ें
- /
- हिंदी पट्टी की...

जब मैंने हिंदी पट्टी की सांस्कृतिक विपन्नता और उनके झूठे दर्प पर पिछली पोस्ट लिखी तो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आईं, जिससे मुझे लगा कि अलग से कुछ बातों को स्पष्ट किया जाना जरूरी है। मेरी पिछली पोस्ट की भाषा में किंचित तीखापन और उलाहना था। जब मैं झूठा दर्प कहता हूँ तो मेरा आशय यही होता है कि आप अपनी सांस्कृति जड़ों के विकृत और बाजारू होने की तरफ आँखें मूंदे हुए हैं और 'संस्कृति' शब्द को एक रेटॉरिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे इन दिनों 'हिंदू संस्कृति' या 'भारतीय संस्कृति' की गहराई में गए बिना उसे एक जुमले की तरह कहीं भी इस्तेमाल कर दिया जाता है।
अगर अतीत का ज्ञान हमारे भविष्य के लिए रोशनी नहीं बनता है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। यूरोप का पुनर्जागरण काल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने अतीत से प्रेरणा ली मगर अतीत की तरफ लौटे नहीं। बल्कि ज्ञान की शाखाओं का उत्तरोत्तर विकास करते गए और निःसंदेह पश्चिम की संस्कृति इस धरती की सबसे प्रभावशाली संस्कृति साबित हुई, इस बात को हमें ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए।
वापस अपनी सांस्कृतिक जड़ों की बात पर लौटते हैं- तो हिंदी पट्टी में हमने जो कुछ भी अच्छा था वो सब छोड़ दिया। पिछली पोस्ट पर कुछ लोगों ने दक्षिण भारत का उदाहरण दिया तो यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि दोनों ही संस्कृतियों में जमीन-आसमान का फर्क है। दक्षिण भारतीयों से हमें सीखना चाहिए कि अपनी भाषा को हेय समझे बिना अंगरेजी को कैसे स्वीकारा जा सकता है और अपनी स्थानीय संस्कृति को छोड़े बिना कैसे अंतरर्राष्ट्रीय हुआ जा सकता है। मैंने कई हिंदी के लेखकों को किंचित गर्व से यह कहते सुना है कि मेरे बेटे-बेटी को हिंदी में रुचि नहीं है। उनके लिए भाषा गर्व का विषय है। हमारे लिए भाषा एक राजनीति है।
मैं बंगलुरु में करीब तीन साल रहा और पाया कि वहां अंगरेजी बोलना स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि आपसी संवाद का जरिया है। एक आटो वाला, एक गृहणी या फिर कोई प्रोफेसर; सभी अपने-अपने तरीके से अकुंठ भाव से अंगरेजी का प्रयोग करते हैं। वहां किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर दस लोग खड़े हैं तो संभव है कि वे छह अलग-अलग भाषा परिवार से आते हों। दक्षिण की भाषाओं में ऐसी समानता नहीं है जैसी हिंदी प्रदेश की बोलियों में है। लिहाजा अंगरेजी सबसे सहज तरीका है आपस में बातचीत का।
दक्षिण की भाषाओं की सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं, खास तौर पर तमिल की। उन्हीं दिनों एक चर्चा में मेरे मलयालम एडीटर ने बताया कि तमिल में अंगरेजी के शब्दों को जस का तस स्वीकारने की बजाय एक नए शब्द का इजाद करने का चलन है। बहुसंस्कृतिवाद का पाठ मैंने बंगलुरू में ही सीखा। मेरे पड़ोस में एक दंपती थे, जिसमें पति तमिल ब्राह्णण था और पत्नी असम की। जाहिर है दोनों की आपसी भाषा अंगरेजी थी। उनके आठ साल के बेटे की भाषा भी अंगरेजी थी और मातृभाषा के नाम पर थोड़ी-बहुत मां की भाषा।
मेरे यहां एक 16-17 बरस की लड़की सुकन्या काम के लिए आया करती थी और वह फर्राटे से अंगरेजी बोलती थी मार्डन स्लैंग्स के साथ। क्योंकि उसने चार साल एक ऐसे दंपती के साथ काम किया था जो उससे अंगरेजी में ही बात करते थे। कुल मिलाकर यह कि वहां की हवाओं में अंगरेजी हावी नहीं बल्कि सहजता से बहती है। दक्षिण भारतीयों का सादगी भरा रहन-सहन, बाहर निकली कमीज और पूरी बांह का सलवार-सूट पहने लड़कियां, गजरे या लंबी चुटिया, खाना खाने का तरीका- कई बार हम उत्तर भारतीयों के लिए उपहास का विषय होता है। पर वे दूसरे अर्थों में आधुनिक हैं। उन्होंने शिक्षा को, सांस्कृतिक विरासत को तथा साइंस और टेक्नोलॉजी को अहमियत दी है।
मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी समाज अपनी संस्कृति को उपादेयता की दृष्टि से देखता है न कि एक जीवन शैली के रूप में। संस्कृति जीवन शैली का हिस्सा कैसे हो सकती है, इसका सबसे सुंदर उदाहरण दक्षिण में लगभग हर घर के दरवाजे पर बनाई जाने वाली सादा सी ज्यामितिक रंगोली है। वहां शादियां दिन में होती हैं। कम खर्च में होती हैं। कोई तड़क-भड़क नहीं, कोई डीजे नहीं। मैंने अपने अनुभव में हमेशा परंपरागत कर्नाटक संगीत ही बजते देखा। लोग आज भी बैठकर केले के पत्तल में ही खाते हैं। मंदिर बहुत साफ-सुथरे हैं। मैंने यहां की तरह किसी मंदिर के आसपास भिखारी को मंडराते नहीं देखा।
इससे यह आशय न निकाला जाए कि वहां सब कुछ अच्छा है और रूढ़ियां नहीं हैं, मगर जो अच्छा है फिलहाल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बंगाली संस्कृति में किताबों, चित्रकला और संगीत का महत्व कितना है यह किसी भी परंपरागत बंगाली परिवार में देखा जा सकता है। करीब तीन साल पहले अर्से बाद मैने गाजियाबाद में दुर्गापूजा पर कालीबाड़ी का कार्यक्रम देखा और पाया कि गीत-संगीत और नृत्य के प्रति उनका प्रेम अभी भी बरकरार है। कुछ भी बदला नहीं है कि आयोजन मुझे किशोरवय में स्मृतियों में ले गया।
हमारे यहां परंपराएं खत्म हो ही हैं और बाजार तेजी से हावी हो रहा है। एक और खास बात यह है कि हिंदी समाज के पास संस्कृति अपने 'लोक रूप' में मौजूद थी। जैसे-जैसे हम सभ्य होते गए हमने 'लोक' को देहाती या पिछड़ा माना और उसे छोड़ते गए। अब खाली जगह को कोई न कोई तो भरेगा, उसे बाजारू और फूहड़ संस्कृति ने भर दिया। पुराने लोक नृत्यों और लोक गीतों की जगह फिल्मी धुनों पर अश्लील गाने बजने लगे। सिनेमा तक में मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज में "हँसि हँसि पनवा खियवले बेइमनवा कि अपना बसे रे परदेस" की जगह "लॉलीपॉप लागेलु" ने ले ली।
लोक को छोड़ने की वजह से उसका परिष्कार नहीं हुआ, जबकि बंगाल और दक्षिण के समाज में उनकी कलाओं का परिष्कार होता चला गया और उन्होंने मध्यवर्ग के जीवन में अपनी जगह ले ली। हिंदी पट्टी में उलटा हुआ। हमें लगा कि आधुनिक होने का अर्थ इन गंवई कलाओं को छोड़ना है। नतीजा हम खाली होते गए अपने खालीपन को हमें एक उथली आधुनिकता से भरना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि हम न तो अपनी संस्कृति से जुड़ पाए और न ही आधुनिक बन सके। आज की तारीख में हिंदी के 'संस्कारी' शब्द का इतना दुरुपयोग हुआ है कि अब यह एक हास्यास्पद शब्द बन गया है।
हम सांस्कृतिक रूप से इतने सूख चुके हैं, बंजर हो चुके हैं कि हम राजनीतिक हिंदुत्ववाद के उभार को भी अपनी पहचान से जोड़ने लगे हैं। हमारे भीतर अपनी संस्कृति के प्रति इतनी हीनभावना बस चुकी है कि उसे श्रेष्ठ बताने के लिए हम सोशल मीडिया या सार्वजनिक जीवन में दूसरों की संस्कृति और पहचान को अपमानित करने या उसका मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं।
धीरे-धीरे हम एक अनुदार और सांस्कृतिक रूप से निर्धन समाज में बदलते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से चाहे कितने भी सपन्न क्यों न हो रहे हों।
(दिनेश श्रीनेत जी की फेसबुक वॉल से)