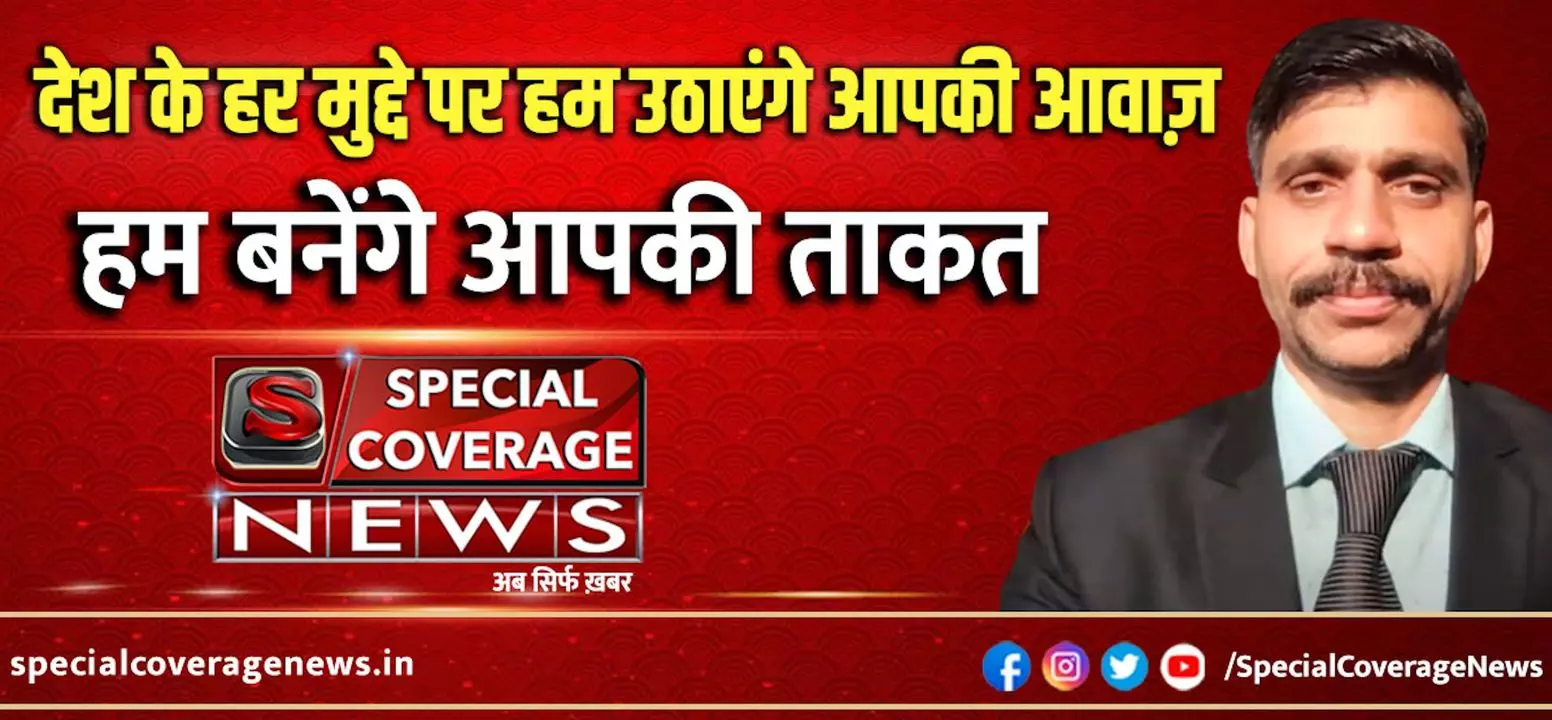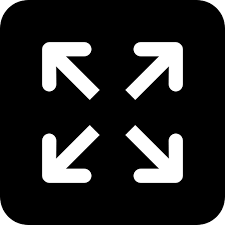- Home
- /
- हमसे जुड़ें
- /
- जहां जीवन ही स्टेक पर...
जहां जीवन ही स्टेक पर लगा हो, वहां पत्रकारिता की किसे पड़ी है?

पत्रकारिता दिवस बीत गया। मेरी आदत है दिन बीतने के बाद लिखना। राडार इसी वक्त खड़ा होता है। मैं सार्वजनिक शुभकामनाएं नहीं देता। न होली की, न दिवाली की, न ईद की, न पत्रकारिता दिवस की। निजी संदेश आते हैं तो सेम टु यू कह देता हूं। शुभ की कामना उसके लिए की जाए जो अशुभ हो। हर व्यक्ति शुभ है। हर दिन शुभ है। हर पर्व शुभ है। पत्रकारिता भी शुभ है। शुभ मानकर ही आए थे इसमें। शुभ मानकर ही अब तक लगे पड़े हैं। अशुभ मानते तो कब का कट लिए होते। वैसे असल समस्या शुभकामना लेने-देने में नहीं, कहीं और है। उसके लिए आपको पत्रकारों (या मोटे तौर पर कलमजीवियों) की जिंदगी में झांकना पड़ेगा। हर शुभ चीज़ के पीछे कुछ न कुछ अशुभ चल रहा है। पत्रकारिता में भी।
हमारे एक मास्टर थे पत्रकारिता के। डॉ. के. एम. श्रीवास्तव। वो कहते थे कि रोटी-कपड़ा तक तो ठीक है, पत्रकारिता करनी है तो मकान की मत सोचना। इंदौर से आते थे पढ़ाने के लिए दिल्ली। हर हफ्ते के अंत में वापस लौट जाते थे। एक दिन पहाड़गंज रेलवे स्टेशन पर गिर गये। फिर नहीं उठे। अशुभ हुआ। पत्रकारों का यही हाल है। मैं तनखैया टाइपिस्टों, स्टेनोग्राफरों या माइकवीरों की बात नहीं कर रहा। वो सब मीडियाकर्मी हैं। जो लिख रहा है, चुन रहा है, बुन रहा है, छांट रहा है, बांट रहा है और किसी की भी नहीं चाट रहा है, वो संभव है पत्रकार हो। उसकी जिंदगी में बहुत कष्ट है। फिर भी वो अपने चुने हुए पर टिका है तो समझिए उसके पीछे कुछ प्रेरणा काम कर रही होगी। जब आप सबको एक तराजू में तौलते हैं, तो उस प्रेरणा पर चोट लगती है।
पत्रकारिता की चिंता में दुबले होने वाले लोगों में से कितनों ने अपने पसंदीदा पत्रकारों से एक बार भी जिंदगी में पूछा है कि बॉस, घर कैसे चलाते हो। पहले पूछते थे लोग। आज से दस साल पहले तक सारी गप करने के बाद लोग पूछ लेते थे, और सब घर में ठीक? चलते-चलते कहते थे, कुछ हो तो बताना। अब नहीं पूछते। लोग सब धान बाइस पसेरी माने बैठे हैं। लिख रहा है तो कमा ही रहा होगा! अजीबोगरीब धारणाएं हैं। अरे? ओला टैक्सी से आया है? गजब गुरु, बहुत पइसा पीट रहे हो! बहुत कुछ है जो समझाया नहीं जा सकता, लेकिन खुद समझ लिया जाए, इसकी चेतना भी अब खत्म हो रही है। इसके अलावा कुछ स्थायी परजीवी संपादक और संस्थान हैं जो बिना कुछ सोचे-समझे फोन लगा देते हैं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। पत्रकारिता के सरोकार का मारा बेचारा पत्रकार वहीं ढेर हो जाता है।
पत्रकारों का खून जितना पत्रकारिता के सरोकार के नाम पर चूसा गया है, उतना मालिकान ने भी नहीं चूसा। जो मालिक से स्वेच्छा से चुसवाते हैं, वो पत्रकार नहीं हैं। उन्हें बोलने का नहीं, मुंह बंद रखने का पैसा मिलता है। आजकल मुंह बंद रखने के लिए पत्रकारिता के नाम पर भी पैसा मिलता है। नये-नये धंधे आ गये हैं। पत्रकारिता के नाम पर पैसा देकर आपको परकटी मुर्गी बना देंगे और आप इस मुगालते में रहेंगे कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि जिसे आप पत्रकार समझ रहे हैं वह किसी कोने में महीन दलाल होता है। फ़र्क धुंधला होता गया है बीते कुछ वर्षों में। इसीलिए पढ़ने-लिखने वाले किसी विवाद की सूरत में तय ही नहीं कर पाते कि किसके साथ खड़ा होना है। मुल्ला नसरुद्दीन वाली हालत हो जाती है। ये भी सही, वो भी सही। इस नैतिक धुंधलके के बीच दलाल अपना काम कर जाता है, पत्रकार मर जाता है।
हम तो गणित को छोड़ पत्रकारिता करने आये थे कि लोगों से कुछ कहेंगे तो वे सुनेंगे, समझेंगे। गणित कौन समझता है इस समाज में? पता चला कि बिना गणित पढ़े ही पत्रकार गुणा-गणित में पारंगत होता गया और समाज सुनने, पढ़ने, समझने से दूर हो गया। अब लिखने के पहले या लिखने के बाद पता ही नहीं रहता कि लेखक की कॉन्सटिचुएन्सी क्या है। जब आपको अपना पाठक ही नहीं पता और पाठक हो भी तो उसे आपसे वास्ता नहीं कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं, तो पत्रकारिता का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सवालों के घेरे में आ जाता है। आज यही हाल है। पाठक और लेखक का सामाजिक अनुबंध टूट चुका है। जैसे नागरिक और लोकतंत्र का। अनुबंध टूट जाए तो सदिच्छा बहुत दिन नहीं खींच सकती।
अभी मैं जोसी जोसेफ को पढ़ रहा था कहीं। उन्होंने लिखा था कि अपने मेल बॉक्स में वे मुर्दाघर नाम से एक फोल्डर रखते थे जहां रिजेक्ट हुई अपनी रिपोर्टें जमा करते जाते थे। बाद में उन रिपोर्टों का उपयोग उन्होंने अपनी किताब में किया। हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा का कौन पत्रकार सोच सकता है कि संपादक द्वारा कचरे में फेंकी गयी स्टोरीज़ से एक किताब बना ले और हार्पर कॉलिन्स से छपवा भी ले? हिंदी के किस पत्रकार को इतनी सहूलियत है कि वह अपना इस्तीफ़ा बाकायदे प्लान करे ताकि उसके निजी उद्यम को तब तक मोटा फंड मिल जाए? अंग्रेज़ी की दिक्कतें भाषायी पत्रकारिता से एकदम भिन्न हैं, गोकि जोसी एक उम्दा रिपोर्टर रहे हैं। पत्रकारिता का संकट किसी रिपोर्टर की स्टोरी रिजेक्ट हो जाने या दबा दिए जाने का संकट नहीं है। उस संकट के मूल में पत्रकारों और पत्रकारिता के प्रति व्यापक समाज में आयी वह बेरुख़ी है जो हर रोज एक पैशनेट पत्रकार को उसके चुने हुए पैशन से हटने पर मजबूर कर रही है; अच्छे रिपोर्टरों को मजबूरीवश अनुवादक बना रही है; अच्छे एडिटर्स को मजबूरीवश एनजीओ के डॉक्युमेंटेशन में धकेल रही है; अच्छे अनुवादकों को टीडीएस काट के बीपी, बवासीर, गैस, मधुमेह का तोहफ़ा दे रही है।
अब चूंकि ठीकरा किसी के सिर फोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें आना अपना चुनाव था, जैसा कि Aman ने आज कहा, तो दो ही रास्ते बचते हैं। या तो अपनी कुर्सी के नीचे कब्र खोद लें या चुपचाप कट लें- कुछ और कर लें। समय रहते संभल लें। वैसे तो बतौर पत्रकार ही क्यों, बतौर मनुष्य भी अब अपनी आइडेंटिटी बदल लेने को जी चाहता है क्योंकि पत्रकारिता का समाज से नहीं, मनुष्यता का भी समाज से अनुबंध टूट रहा है। क्या कोई जुगत लग सकती है कि लगे हाथ कोरोना के खेल में अपना नाम भी शामिल करा लिया जाय .....? और आप समझ रहे हैं में कहना क्या चाह रहा हूँ? आजकल मेरे मित्र अंकुर के बीच ऐसी ही संभावना पर बात हो रही है।
जहां जीवन ही स्टेक पर लगा हो, वहां पत्रकारिता की किसे पड़ी है?