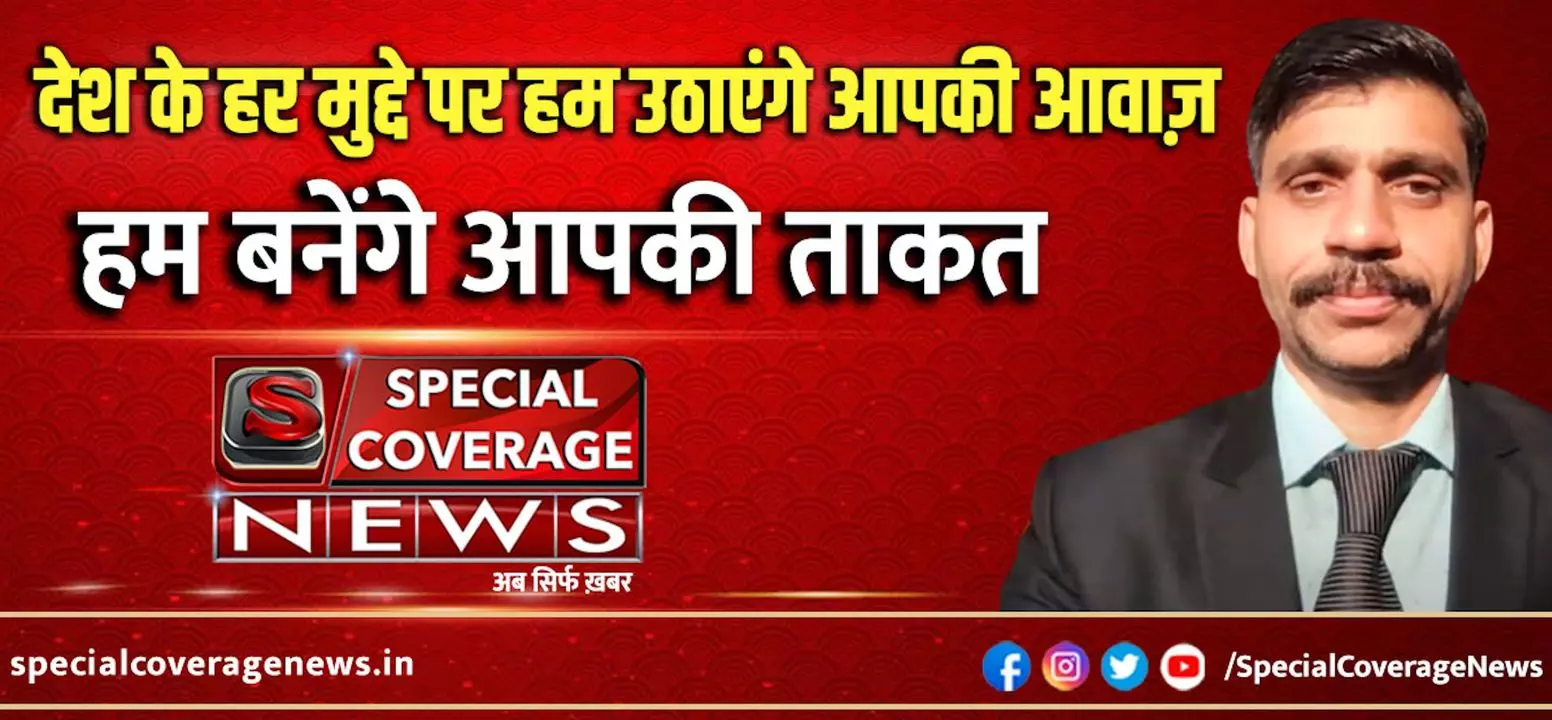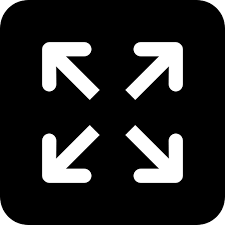अब और कितना विकास चाहते हो, 'हे मानव संसाधन....'
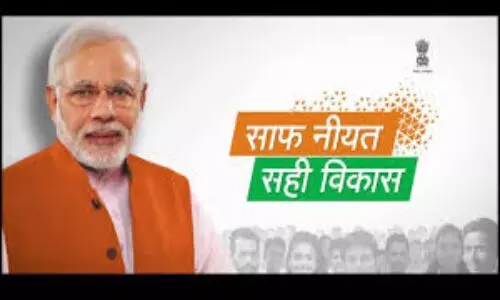
विजय शंकर पाण्डेय
कोरोना डेटा अब अखबारों, न्यूज चैनलों और पोर्टलों के लिए स्कोर बोर्ड सरीखा है. इतने विकेट पर इतने रन. नो बॉल इतने, जीवन दान इतनी बार, वाइड बॉल वगैरह वगैरह. ब्रीफ में चाह दे तो दो लाइन में पूरी इंडिया समेट दें. आप बस तालिका को स्क्रॉल करते जाइए. हो सकता है एक दिन कोई इत्मीनान से गहरी सांस लेते हुए कह दें कि चलो भाई, 136 करोड़ की आबादी में एक दो फीसदी लोग नहीं रहे... आप बोर न हो, इसलिए चीयर्स के लिए बीच बीच में यह भी खबरें आएंगी कि बॉलीवुड के शहंशाह ने कितनी बार करवट बदली. उन्हें अच्छी नींद आई या नहीं. अब और कितना विकास चाहते हो, हे मानव संसाधन.... कई बार लगता है कि हम 'विकास' के चरम उत्कर्ष के दौर में पहुंच गए हैं. वाकई ऐसा है? या अब भी दिल्ली दूर है?
शुरुआत 'विकास' के बेबी पैक से ही करते हैं. पहले तो सीबीएसई 12वीं की आल इंडिया ऑफिशियल टॉपर दिव्यांशी जैन और तुषार सिंह को बधाई. मुझे इन बच्चों की प्रतिभा पर तनिक भी शक नहीं है. मगर इस तरह की उपलब्धियों का एक ऐंगल यह भी है कि हम बंद गली के आखिरी मकान के सामने खड़े हैं. मुझे हैरत हुई कि इनकी कॉपियों पर किसी परीक्षक ने 'The Examinee is better than Examiner' जैसी टिप्पणी लिखने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा सका? क्योंकि इससे बेहतर परफॉरमेंस और क्या हो सकती है? जाहिर है, परीक्षक या तो ईमानदार नहीं था, या फिर इनके टैलेंट के आगे उसका कॉन्फिडेंस जवाब दे गया. या फिर उस टीचर के लिए अप्रत्याशित या असंभव जैसी कोई घटना ही नहीं घटी हो, जिसके चलते वह बाध्य होकर इस तरह की टिप्पणी करता. जबकि उन टीचरों के मुकाबले इन बच्चों का नंबर प्रतिशत कहीं बेहतर है, तभी न इतिहास रचे जैसी हेडलाइन मीडिया इस्तेमाल कर रही है
यह हमारी शैक्षणिक व्यवस्था पर भी सवाल है. हो सकता है राजेंद्र प्रसाद पिछड़े भारत के दौर की प्रतिभा थे, तब ऐसी बातें उपलब्धि हुआ करती होंगी. हमारे दौर तक एक गुड सेकेंड डिविजन भी हुआ करता था, अब तो फर्स्ट डिविजन की भी चर्चा नहीं होती. बात शुरू ही होती है 90% या उससे ऊपर से. तो सोचिए कि इसके आगे की लड़ाई कितनी भीषण होने वाली है. और जरा उन बच्चों के बारे में भी सोचिए कि जो 90% से नीचे हैं. कैसी मनःस्थिति होगी उनकी और उनके माता-पिता की? यह भी मत भूलिएगा कि मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, माइकल डेल, स्टीव जॉब्स, रितेश अग्रवाल, कुनाल शाह और कैलाश खट्टर वगैरह वगैरह भी इसी लोक के प्राणी हैं, एलियन तो कत्तई नहीं हैं.
अभी हाल ही में टाई सूट-बूट में सजे एक नौजवान ने मेरी डोर बेल बजाई. मैं बॉलकनी से ही किसी अपरिचित को देख कर पूछा – बताओ भाई, क्या बात है? जवाब मिला – सर, जरा नीचे आइए न, आपसे कुछ बात करनी है. मैंने पूछा, भइया दोपहर के ढाई बज रह हैं, मुझे खाने पर बुलाया गया है. आप वजह बताइए, वाजिब लगेगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा अथवा मुझे खाना खाने जाने की इजाजत दीजिए. उस लड़के ने मन मसोसते हुए कहा कि एक खास प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं. मैंने जवाब दिया – मान्यवर इस कोरोना काल में दो वक्त की रोटी के अलावा गमछा तक नया नहीं खरीदा गया. इसलिए किसी भी अन्य प्रोडक्ट पर चर्चा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता. असल में कई प्राइवेट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग स्कूल बनारस समेत पूरे देश में खुल गए हैं. कायदे का मौका गिने चुने के ही हाथ लगते हैं. बाकी सेल्स मैनेजर का आईकार्ड लेकर सेल्स मैन की भूमिका में आ जाते हैं. कानपुर में मेरे एक पड़ोसी का बेटा उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में 12,000 की चाकरी करता था, जहां से उसने डिग्री ली थी.
मेरे एक मित्र और वरिष्ठ टीवी पत्रकार की बिटिया ने भी इंटर अच्छे नबर से पास किया है. वह डॉक्टर बनना चाहती है. व्यक्तिगत बातचीत में मेरे मित्र ने साफ साफ कहा कि पांडेय जी, अगर वह कॉम्पिटिशन पास कर किसी सरकारी कॉलेज में दाखिला पा जाती है, तब तो मर जीकर पढ़ा दूंगा. अन्यथा करोड़ों रुपये फूंक कर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाना मेरी समझ से मूर्खता होगी. उनकी दो टूक राय है कि जो बच्ची करोड़ों फूंक कर डॉक्टर बनेगी, सोचिए वह कितनी निर्दयता से उस पैसे का रिटर्न चाहेगी. और क्यों न चाहे? मगर यह तो पाप ही होगा न? ऐसे डॉक्टर बनने से तो बेहतर है कि करोड़ों फूंक पहले ही कायदे का जनरल स्टोर खोल दिया जाए. बिना खून चूसे आजीवन रोजी रोटी की गारंटी तो रहेगी. फिर एक सामान्य पत्रकार के लिए करोड़ों जुटाना भी तो एक समर ही है. कई बार मुझे लगता है कि रिजल्ट के इस बदले पैंतरे में भी झोल ही झोल है.
उन दिनों मैं लखनऊ के एक अखबार का मुलाजिम था. लखनऊ की कोई लड़की किसी लिटिल चैम्प टाइप टीवी प्रोग्राम के फाइनल में पहुंच चुकी थी. अब उसका मुकाबला असम की किसी प्रतियोगी से था. दोनों उस स्टेज में थीं जब पब्लिक वोट बहुत मायने रखता था. हमें भी अपनी खबर बेचनी थी. स्वार्थ ही तो हम भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ता है. वरना कितना प्रेम है आप जानते ही हैं. हो सकता है मुझसे ही कल कोई 'पांडेय जी' पूछ बैंठे कि भइया पांडेय हो..... यह तो फेसबुक पर प्रोफाइल देख कर ही पता चल गया, मगर कौन से पांडेय हो? इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला ऐंगल जरूरी था. एडिटोरियल की बैठक में तय हुआ कि खबर को इस अंदाज में परोसा जाए कि यूपी की पहली बेटी इस मुकाम तक पहुंची है, इसलिए हिंदी भाषी लोग उसे वोट जरूर करें. प्रदेश की इज्जत का सवाल है. आप जानते ही हैं, नाक ही धाक होती है. क्योंकि बाकी तो ठन ठन गोपाल हैं.
हालांकि मुझे और मेरे पत्रकार साथियों को पहले से ही अनुमान था कि बाजी असम की लड़की के हाथ ही लगेगी. इस वजह से नहीं कि लखनऊ वाली लड़की किसी मायने में अपने प्रतिद्वंद्वी से कमतर थी, बल्कि उसकी मूल वजह मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी. प्रोग्राम आप हिंदी में पेश कर रहे हैं. गैर हिंदी भाषी राज्यों के लोग उसे क्यों देखें? कोई तो वजह होनी चाहिए. हिंदी भाषी तो उस प्रोग्राम को देखेंगे ही, क्योंकि चुनावी भाषा में वे उसके डेडिकेटेड वोटर या वोट बैंक मान लिए गए हैं, मगर गैर हिंदी भाषी लोगों को तुष्ट करके ही वहां बिजनेस मार्केट को विस्तार दिया जा सकता है. प्रकारांतर में आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि वहां परीक्षा कॉन्टेस्टेंट की नहीं, कॉंन्टेस्ट की ही होनी थी. अर्थात प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सस्पेंस और थ्रिल का फुलटॉस तड़का जरूरी था. हमारा अनुमान अक्षरशः सही निकला, विजेता असम की लड़की हुई. लखनऊ वाली कॉन्टेस्टेंट की कार यूपी में दाखिल होते ही पलट गई.
विकास दुबे की कार का यूपी में क्या हस्र होना था? सोशल मीडिया पर घटना से एक दिन पहले के पोस्टों को देखिए तो ज्यादातर लोग इत्मीनान से प्रेडिक्ट कर रहे थे. या फिर हालात ऐसे बना दिए गए या बनवा दिए गए कि नतीजे पर पहुंचना किसी के लिए भी आसान हो चुका था. और अप्रत्याशित कुछ हुआ भी नहीं. कसाब या निर्भया के गुनहगारों के प्रति इस देश में सहानुभूति शायद ही किसी को हो, मगर आतंकी या दुष्कर्मी का जवाब देने के लिए हमारा सिस्टम आंख के बदले आंख के पैटर्न पर नहीं चला. मुर्दे पर लाठी भांजने में पूरे विश्व में हमारी मीडिया का कोई तोड़ नहीं है. अब एक से बढ़कर एक स्टोरी सामने आ रही है.
बीते दो दशक से तो मैं यूपी की पत्रकारिता को काफी करीब से देख, सुन, समझ और जान रहा हूं. मगर विकास को लेकर कई रहस्योद्घाटन मेरे लिए भी अब हो रहे हैं. इन्हीं में से एक है सीओ देवेंद्र मिश्र से 22 साल पुरानी थी विकास की रंजिश... पहले भी वे एक दूसरे पर फायरिंग कर चुके थे. मगर दोनों बच गए. देवेंद्र मिश्र कुछ नहीं कर सके, क्योंकि राजनीतिक दबाव था. तो भइया इस तरह की ढेर सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को बीसेक साल पहले ही छाप दिए होते. अब छापने का एक मतलब तो यह भी है कि मीडिया आठ पुलिसकर्मियों की शहादत का इंतजार कर रही थी. अगर नहीं तो मुर्दे पर लाठी भांज किसे क्या बताना चाह रहे हों? आजकल रोज नई स्टोरी ऐसे निकल रही है गोया बर्रे के छत्ते में किसी ने ढेला फेंक दिया है. जाहिर है इसके जरिए आप कोई बात साबित करने पर तूले हैं. इसी बीच कोई न कोई यह सफाई भी देता फिर रहा है कि ब्राह्मणों का नेता नहीं था विकास. यह बताने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? या आप सफाई दे रहे हैं, मगर किसे? और क्यों? कोई मीडिया या सोशल साइट के अड्डेबाजों की बात क्यों मान ले?
अपराध और राजनीति का कॉम्बिनेशन यूपी और बिहार को ले डूबा. इसमें दूध का धूला कोई नहीं है. सच्चाई तो यह है कि अपराधियों के बगैर यहां राजनीति की ही नहीं जा सकती. पहली बात तो यह है कि चुनाव को सुनियोजित ढंग से इफरात पैसों के खेल में तब्दील कर दिया गया. साथ में आपराधिक छवि से एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाता है तो कोई तोड़ रह नहीं जाता.
"न ही लक्ष्मी कुलक्रमज्जता, न ही भूषणों उल्लेखितोपि वा. खड्गेन आक्रम्य भुंजीतः, वीर भोग्या वसुंधरा." अर्थात न तो लक्ष्मी निश्चित कुल से क्रमानुसार होती है और ना ही आभूषणों पर उसके स्वामी का चित्र अंकित होता है. खड्ग व शक्ति के बल पर पुरुषार्थ करने वाले ही विजयी होकर रत्नों को धारण करने वाली धरती को भोगते हैं. राजनेता और धर्म गुरु जब भी आपको यह श्लोक सुनाते हैं तो सिर्फ "वीर भोग्या वसुंधरा" बताते हैं, बाकि गोल कर जाते हैं.
यूपी और बिहार में आज भी वोट लेने के लिए कम से कम चार नाल राइफल, अब एके 47 और एसयूवी का काफिला अनिवार्य शर्त है. इसीलिए यहां हर जिले में दो चार ऐसे विकास हैं, जो "विकास" के चरम उत्कर्ष तो पहुंचने को आकुल व्याकुल हैं. बहुतेरे पूरी कामयाबी से शिखर चूम भी रहे हैं.
शुरुआत में व्यापारी सदनों में अपने प्रतिनिधि भेजा करते थे. बाद में उन्हें खुद वहां का शोभा बढ़ाना किफायती सौदा लगने लगा. सीधे आम चुनाव में लड़ने में दिक्कत है, तो राज्य सभा या विधान परिषद में बैकडोर से बिना किसी लफड़े के एंट्री मिल जाती है. पैसे की जरूरत हर राजनीतिक दल को है, इसलिए टिकट मिलना आसान है. जाहिर है प्रत्यक्ष या परोक्ष टिकट हर पार्टी बेचती है, बदनाम कुछ खास लोगों को ही सुनियोजित ढंग से किया जाता है. इसी तर्ज पर अपराधी भी अब सीधे वहां पहुंचने लगे हैं. वहां पहुंच जाने के बाद सारे मुकदमों से मुक्ति मिलने के द्वार खुल जाते हैं.
विकास दुबे अपने हिसाब से करियर ही बना रहा था. मगर कइयों का करियर उसे निपटाकर बन और बच गया, वरना औंधे मुंह गिरते. कलेजे पर हाथ रख कर कहिए कि क्या बगैर राजनीति, पुलिस की मदद के विकास दुबे चौबे बनने निकला था? गौर से अगर यूपी और बिहार की राजनीति को देखिए सारा खेल दबदबा और पैसे का ही तो है.
जौनपुर जा रहा था किसी की बारात में. वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर भीषण जाम था. घटना चार पांच साल पुरानी है. तब रिंग रोड बनना शुरू ही हुआ था. ड्राइवर गली कूचों से होकर निकलने लगा. मैं कहा कि भइया अन्जाने इलाके से ले जा रहे हो. कहीं रात भर घुमाते ही मत रह जाना.
ड्राइवर ने आश्वस्त किया, नहीं साहब, निश्चिंत रहिए. हम लोग रिंग रोड के करीब है. मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं.
मैंने कहा, यार आप लोगों के इलाके में तो बहुत पैसा आया होगा. रिंग रोड बनने से काफी पैसा मिला है यहां के लोगों को. आसपास के जमीनों की कीमतें भी बढ़ गई.
हां, साहब, इधर जिसकी जमीन थी, उसकी तो लॉटरी निकल गई.
एकमुश्त इतना पैसा आया है तो इधर के लोगों की लाइफ स्टाइल बदल गई होगी?
साहब ठीक ठाक जिन्हें पैसा मिला है, उनमें ज्यादातर लोगों ने महंगी लग्जरियस कारें खरीदी और असलहे.
जाहिर है कुछ पैसा आया तो यहां के लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर सेक्टर पॉलिटिक्स समझ में आया. ताकि रिटर्न भी वैसा ही धमाकेदार मिलता रहे. साथ में सोशल स्टेटस भी.
वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर की एक टिप्पणी किसी अखबार के एडिट पेज पर छपी थी. लब्बोलुआब यह था कि भारतीय राजनीति में जो पकड़ा गया वह चोर है, जो महारथी बच बचा कर बाजी मार ले गया, वह साधु है.
लॉकडाउन शुरू हुआ तो मजदूरों की घर वापसी भी शुरू हो गई. देश भर की मीडिया में सुर्खियों में यूपी और बिहार था. हर ऐसे नाजुक मोड़ पर यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर यूपी और बिहार के लोगों को रोजी रोटी यहां क्यों नहीं मिल सकती? जवाब यही है कि यहां कोई भी बड़ा इंडस्ट्रलिस्ट पैसा लगाने से हिचकता है. अनआफिशियली कानून व्यवस्था, लचर बिजली आपूर्ति और लालफीताशाही का रोना रोया जाता है. बीते दो दशक से तो हर चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े जाते हैं. मगर स्थितियां सिर्फ प्रेस विज्ञप्तियों और विज्ञापनों में बदलती दिखती हैं. लौटे मजदूरों को अब यूपी से बाहर नहीं जाने देंगे? मगर किसके बूते? मनरेगा के बूते? क्या आपको ऐसा संभव लग रहा है?
कई बार तो लगता है विकास करते करते हम 600 में 600 अंक हासिल कर लिए हैं. अब उससे आगे एक नंबर भी नहीं पा सकते, गड्डी अब रिवर्स गियर में ही चल सकती है.