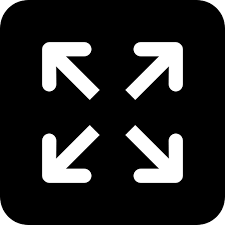रामलीला: संस्कृति की दहलीज़ से साम्प्रदायिकता के शिखर तक

साम्प्रदायिकता की आंधी इतनी प्रबल और आक्रामक थी कि विरोध के उनके स्वर ज़्यादा टिक नहीं सके। ऐसे दौर में जबकि समूचा देश कोविड19 की चपेट में बेतरह त्रस्त है, अखिल भारतीय स्तर पर इनकी प्रस्तुतियों को रद्द करने का निर्णय लिया गया। यह एक सही निर्णय था। तब सवाल उठता है कि अयोध्या और दिल्ली में इन्हें प्रस्तुत किये जाने की अनुमति क्यों दी गई?
कोरोना से उपजे एहतियात के चलते दिल्ली, अयोध्या के अपवाद को छोड़कर समूचा देश इस बार रामलीलाओं का आनंद उठाने से चूक जाएगा। हिंदी कैलेण्डर के अश्विन मास के दौरान देश के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के अधिकांश भागों में रामलीलाएँ सैकड़ों सालों से एक शानदार, विराट, अभूतपूर्व और मनोरंजक सांस्कृतिक परिघटना होती रही है। शताब्दियों से यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बहुजातीय और बहुनस्लीय विराट चिंतन का प्रतिनिधित्व करती आई है। आज भी इनकी अंतरात्मा लोकपक्षीय बनी रहने के बावजूद आख़िर इनके आँचल पर संकुचित विचारों का भारी-भरकम रंग कैसे चढ़ गया है, यह सोचने की बात है।
यद्यपि इस बात का कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है लेकिन यह एक आमफ़हम मान्यता है कि सबसे पहली रामलीला 17वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास के शिष्य मेघा भगत ने चित्रकूट में खेली थी। जहाँ तक दस्तावेज़ों का सवाल है पहली रामलीला होने का उल्लेख वाराणसी के रामनगर में सन् 1830 में मिलता है। इसके प्रवर्तक तत्कालीन काशी नरेश महाराजा उदितनारायण सिंह थे। बनारस के मीलों लंबे इलाक़े को 'लीला' के प्रदर्शन स्थल के रूप में विकसित किया गया। अलग-अलग जगहों पर 'अयोध्या' 'वनवास' और 'लंका' कांड प्रदर्शित होते। 'यूनेस्को' के मुताबिक़ बनारस के रामनगर की रामलीला अभी तक चलने वाला संसार का एक मात्र लोकनाट्य है, जहाँ प्रदर्शन स्थल अलग-अलग स्थानों पर होते हैं और दर्शक घूम-घूमकर इन प्रदर्शनों का लुत्फ उठाते हैं। इसके बाद के दशकों में समूचे उत्तर भारत में रामलीलाओं की बाढ़ आ गई।
आगरा की रामलीला 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में शुरू की गई। इसी दौरान अयोध्या, वृंदावन, अल्मोड़ा, सतना, मधुबनी आदि स्थानों पर लीलाओं का चलन शुरू हुआ।
दिल्ली की प्रसिद्ध रामलीला की शुरुआत अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह 'ज़फ़र' के जमाने से हुई। बादशाह प्रायः इसकी प्रस्तुतियों का आनन्द उठाने पहुँच जाया करते थे।
इसे यद्यपि रामलीला कहकर नहीं पुकारा जाता था लेकिन सन 1610 में 'मैसूर दसारा' नामक जिस दशहरा उत्सव की शुरुआत मैसूर (कर्नाटक) में हुई थी, वह आज तक शानदार तरीक़े से मनाया जाता है। दक्षिण भारत के लोगों के समक्ष यह रामकथा के अनंत स्वरूप का विस्तार है। उत्तर भारत में जहाँ दशहरा रामलीला के समापन के रूप में अंतिम (एक) दिन मनाया जाता है, वहीं 'मैसूर दसारा' दस दिन चलने वाला एक विशाल समारोह है। इस दिन यह उत्सव समूचे राजसी मैसूर को अपने आग़ोश में ले लेता है। शहर के ढेर से ऑडिटोरियम, मैसूर पैलेस, प्रदर्शनी ग्राउंड, महाराजा कॉलेज ग्राउंड और चामुंडी हिल पर यह समान रूप से मनाया जाता है।
उत्तर भारत में रामलीला की शुरुआत एक छोटे से धार्मिक अनुष्ठान के रूप में की गई थी। इसके दर्शक रामभक्त होते थे, और प्रस्तुति देने वाले कलाकार भी। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों के तुष्टिकरण के तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने जो अनेक सुधारात्मक कार्रवाईयाँ की थीं उनमें रामलीलाओं के लिए समुचित बड़े मैदान मुहैया कराना व इससे जुड़े दूसरे इंतज़ामों में सहयोग करना शामिल है।
अपनी शुरुआती समझ में अंग्रेज़ भी इसे हिन्दुओं के धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखते थे, लेकिन जैसे-जैसे इन लीलाओं के प्रदर्शन का इतिहास लंबा होना शुरू हुआ, इनके प्रदर्शन के लिए खुले और बड़े स्थान उपलब्ध होने लगे। इनकी लोकप्रियता का ग्राफ़ बढ़ने और इनके धर्म से ऊपर उठकर एक बड़ी सांस्कृतिक परिघटना के रूप में परिवर्धित होते चले जाने की कथा क्रमवार है। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध के चरम तक पहुँचते-पहुँचते देश के अनेक स्थानों पर दूसरे धर्मों के मतावलंबी भी इसमें शरीक होने लगे। यद्यपि 20वीं सदी के शुरुआती दशकों तक उनका यह जुड़ाव महज दर्शक के रूप में था।
जैसे-जैसे समय गुजरा लीलाओं में नाटकीयता बढ़ती गई।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ज़्यादातर स्थानों पर होने वाली इन लीलाओं में पारसी नाटक परम्परा बेतरह अपना असर डालने लगी थी। बेशक अधिकांश प्रदर्शनों का आधार गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयाँ और दोहे हुआ करते थे लेकिन शुरुआती सपाट चेहरों वाले प्रस्तुतिकर्ताओं की तुलना में बाद के अभिनेताओं के 'भाव'अधिक परिपक्व होते चले गए। अब चेहरे उनके भावों के उतार-चढ़ाव का स्पष्ट प्रदर्शन करते और उनके शरीर, गतियों और अभिनय से लबरेज़ होते थे। ऐसी नाटकीयता प्रधान लीलाओं ने विराट दर्शक वर्ग का मनोरंजन करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि दोपहर बाद से सरेशाम तक चलने वाली इन प्रस्तुतियों में दर्शकों के रूप में हिन्दू भी होते, मुसलमान, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई भी।
अनेक प्रस्तुतियों में अंग्रेज़ अधिकारी भी अपने परिवारों के साथ दर्शक के रूप में मौजूद होते। पहली सहस्त्राब्दि के बाद के मध्यकाल में जिस तरह की गंगा-जमुनी तहज़ीब भारत में विकसित हुई, वहाँ देखते-देखते रामलीला सभी धर्म वालों का प्रधान मनोरंजन बन गई।
ब्राह्मण पुत्रों के अलावा आगे चलकर दूसरे सवर्ण और पिछड़ी जातियों के बच्चे भी लीलाओं में अभिनेता बनने लगे। कालांतर में अनेक स्थानों पर दूसरे धर्मावलंबी (सिख, मुसलमान, ईसाई आदि) भी लीला का हिस्सा बन गए। छोटे-छोटे गाँवों और क़स्बों से लेकर बड़े-बड़े शहरों वाले समूचे देश के अनेक स्थलों में यह सिलसिला अभी भी जारी है। इस तरह देखते-देखते 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रामलीलाएँ धर्मनिरपेक्ष भारत का सजीव प्रतिनिधित्व करने लगीं।
सांप्रदायिकता का रंग कैसे चढ़ा?
श्रीराम वैदिक धर्म के सच्चे उपासक माने जाते हैं। उनका चिंतन इतना विराट था कि अपनी सेना में उन्होंने न सिर्फ़ गैर हिन्दू बल्कि ग़ैर मानव नस्लों को भी तरजीह दी। रीछ और वानरों की उनकी विशाल फौजों ने न सिर्फ़ लंका का क़िला ध्वस्त किया बल्कि दुराचारी रावण और उसके सहयोगियों का संपूर्ण नाश कर डाला। अपनी शुरुआत से लेकर आज तक देश भर की रामलीलाएँ राम के इसी विराट चिंतन का प्रतिनिधित्व करती आई हैं। 1980 के दशक में उपजे बाबरी मसजिद-रामजन्म भूमि विवाद के बाद से राम के व्यापक सांस्कृतिक व्यक्तित्व और कृतित्व को धर्म और साम्प्रदायिकता के संकुचित खाँचे में 'फ़िट' करने की कोशिशें शुरू हुईं। जब उनकी गाथा से जुड़ी धरती का ही राजनीतिकरण कर दिया गया तो भला उनसे जुड़ी कथा, किंवदंती, साहित्य और सांस्कृतिक मूल्य कैसे बचते। नतीजा यह हुआ कि रामलीलाओं को भी सांप्रदायिक रंगों में रंगने की कोशिशों का सिलसिला शुरू हुआ।
दिल्ली की ऐतिहासिक रामलीलाओं में दशहरा या अन्य उत्सवों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन विभूतियों के जाने की परंपरा रही है लेकिन जब बीजेपी प्रमुख या शीर्ष पदों पर विराजमान नेताओं के रूप में आडवाणी या अटलबिहारी वाजपेयी के पहुँचने और वहाँ धनुष उठाकर बाण छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि सांस्कृतिक रामलीला को अब राजनीतिक रंग देने से कोई नहीं रोक सकता। सन 90 के बाद यह प्रक्रिया निरंतर तेज़ होती चली गई।
'रामलीला कमेटियों' में 'संघ' परिवार
उत्तर भारत की ज़्यादातर 'रामलीला कमेटियों' में 'विश्व हिंदू परिषद' के बहाने 'संघ' परिवार क़ाबिज़ होना शुरू हो गया। इन 'कमेटियों' में जो सेक्युलर विचारों वाले बुज़ुर्ग सदस्य थे उनके ख़िलाफ़ 'आयु सीमा' के नाम पर ऐसा मोर्चा बनाया गया कि वे ख़ुद छोड़ कर चले जाएँ। यूपी, एमपी, हरियाणा और हिमाचल में बड़ी तादाद में पुराने कांग्रेसी थे, उन्हें निकाल बाहर किया गया। इनके स्थान पर बीजेपी ने अपने सांसद और विधायकों को बैठा दिया। राजस्थान में अलबत्ता वे पूरे तौर ऐसा कर पाने में क़ामयाब नहीं हो सके। इसके बाद 'जय श्रीराम' के उद्घोष की शुरुआत के साथ 'वीएचपी' के बाक़ी एजेंडे की एंट्री करवाई गई। रामलीला मंच के बहुरंगी 'विंग' और पर्दों को नारंगी रंग में रंग दिया गया।
श्रीराम आरती के नाम पर शहरों के बीजेपी और 'संघ' परिवार के पदाधिकारियों को मंचों पर आमंत्रित किया जाने लगा। ये लोग आते और 'आरती' के बाद के अपने उद्बोधन में राम जन्मभूमि की स्थापना के महत्व पर लंबे-लंबे आख्यान देकर माहौल 'गरमाते'।
आगे चलकर बहुत सारी जगहों पर रामलीलाओं को 'सेंसर' किया गया। पीढ़ियों से इनमें अभिनय करने वाले ग़ैर सवर्ण और ग़ैर हिंदू कलाकारों को, जो अभिनय में पारंगत और अपनी भूमिकाओं में धुरंधर हो चुके थे, हटा दिया गया और उनकी जगह 'हिंदू' और 'ब्राह्मण' पुत्रों को लाया गया। रंगमंचीय दृष्टि से इनमें अधिकांश अज्ञानी और कूढ़मग़ज़ थे। स्वभावतः ऐसा करने से इन 'लीलाओं' का रंगमंचीय और कलात्मक स्तर नीचे गिरता चला गया। सैकड़ों सालों की शानदार रंगमंचीय परिपाटी और ऐतिहासिक रामकथा को सांप्रदायिकता के घृणित पिंजरे में क़ैद कर डालने को आतुर राजनेताओं को इसके कलात्मक स्वरूप से क्या लेना-देना था?
चूँकि यह सैकड़ों सालों की स्थापित सांस्कृतिक परिपाटी थी लिहाज़ा अनेक स्थानों पर इनका जम कर विरोध हुआ। इन कोशिशों का ऐसे लोगों ने भी विरोध किया जो बिलानागा सुबह सवेरे घर में या कम्युनिटी स्थलों पर जाकर 'मानस' का पाठ किया करते थे। 'खांटी हिंदू' या 'सनातनी' होने के बावजूद गंगा-जमुनी तहज़ीब उनके भीतर का एक स्वाभाविक सांस्कृतिक बोध थी इसलिए वे विरोध को निकल पड़े।
साम्प्रदायिकता की आंधी इतनी प्रबल और आक्रामक थी कि विरोध के उनके स्वर ज़्यादा टिक नहीं सके। ऐसे दौर में जबकि समूचा देश कोविड19 की चपेट में बेतरह त्रस्त है, अखिल भारतीय स्तर पर इनकी प्रस्तुतियों को रद्द करने का निर्णय लिया गया। यह एक सही निर्णय था। तब सवाल उठता है कि अयोध्या और दिल्ली में इन्हें प्रस्तुत किये जाने की अनुमति क्यों दी गई?
साहित्य, कला, सांस्कृतिकता और मनोरंजन की दहलीज़ से चलकर रामलीला कैसे साम्प्रदायिकता की दीवार पर रेंगती कुत्सित राजनीति के शिखर तक पहुँची है, इसे देखना तो दुखद है ही, यह हमारी परंपरा और मूल्यों के विनाश का भी द्योतक है। जिस तरह की सांस्कृतिक साझा विरासत देश भर की रामलीलाएँ परोसती आई हैं, ज़रूरत उन्हें सहेज कर रखने की है। नवरात्रों के उपवासों में तमाम संकल्पों के साथ हम यदि इस साझा विरासत को सुदृढ़ करने का संकल्प भी लेते हैं तो यह राम और विजयदशमी- दोनों के प्रति हमारे सच्चे विश्वास का प्रतीक सिद्ध होगा।
साभार सत्य हिंदी डॉट कॉम