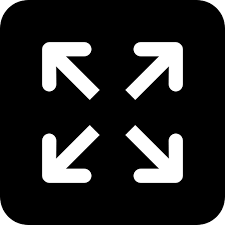मुहम्मद अली शाह शुएब
इस्लाम में त्यौहार की हैसियत
इन्सान ने जब से मुआशरती व तमद्दुनी ज़िन्दगी (सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन) गुज़ारना शुरू की है, तक़रीबन उसी वक़्त से अपनी ख़ुशी का इज़हार करने के लिए वो कुछ त्योहार मनाता चला आ रहा है। मानो ख़ुशियाँ मनाना इन्सान की फ़ितरत (स्वभाव) है। इन्सान की इसी फ़ितरी ख़ाहिश के पेशे-नज़र (परिप्रेक्ष्य में) इस्लाम ने दो त्योहार रखे हैं। ईदुल-फ़ित्र और ईदुल-अज़हा या बक़रईद। (यहाँ ये बात वाज़ेह तौर (स्पष्ट रूप) से समझ लेने की है कि इन दो त्योहारों के अलावा इस्लाम में कोई और त्योहार नहीं है। यानी शबे-बरात, मुहर्रम, ईद-मीलादुन्नबी वग़ैरा न तो त्योहार हैं और न इनकी कोई इस्लामी मान्यता या महत्व है।)
इन दोनों त्योहारों में से पहला तो मनाया जाता है रमज़ान के रोज़े पूरे होने की ख़ुशी में और इस बात की ख़ुशी में कि अल्लाह ने इसी महीने में तमाम ही इन्सानों की हिदायत (मार्गदर्शन) के लिये एक मुक़द्दस (पवित्र) किताब क़ुरआन नाज़िल की। दूसरा त्योहार यानी ईदुल-अज़हा उस बेमिसाल क़ुरबानी की याद में मनाया जाता है जो अब से क़रीब चार हज़ार साल पहले ख़ुदा के एक सच्चे पैरौ और मुतीअ (भक्त और आज्ञापालक) हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने अपने मालिक के हुज़ूर (समक्ष) पेश फ़रमाई थी। जिस तरह ईदुल-फ़ित्र मुहम्मद (सल्ल०) की पैग़म्बरी की यादगार और नुज़ूले-क़ुरआन का जश्न है उसी तरह ईदुल-अज़हा बाबा इबराहीम (अलैहि०) की सुन्नत (तरीक़े) की यादगार और दीने-इस्लाम के मुकम्मल हो जाने का जश्न है, क्योंकि इसी दिन क़ुरआन की वो आयत नाज़िल हुई थी जिसमें अल्लाह ने कहा था कि-
"आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से पसन्द किया।" (क़ुरआन सूरा-5, अल-माइदा, आयत-3) दीन के मुकम्मल होने के पहलू से ईदे-क़ुर्बाँ की अहमियत यूँ है कि ये उस ख़ास वाक़िए की सालाना यादगार है जब दीन 'इस्लाम' की शक्ल में मुकम्मल हो गया और पूरी नौए-इन्सानी (मानव जाति) की दुनिया व आख़िरत (लोक-परलोक) की कामयाबी हमेशा के लिए इसी दीन 'इस्लाम' की पैरवी में रख दी गई। लेकिन इस ईद की अहमियत को और ज़्यादा वसी मानों (व्यापक अर्थों) में समझने की ज़रूरत है। ईदुल-अज़हा के मौक़े पर पूरी दुनिया के मुसलमान जानवरों की क़ुरबानी करके बाबा इबराहीम (अलैहि०) की उस बेमिसाल क़ुरबानी की याद ताज़ा करते हैं जिससे बड़ी क़ुरबानी की मिसाल दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। इस पूरे वाक़िए को समझने से पहले हमें सबसे पहले क़ुरबानी का मतलब और उसके मक़सद (उद्देश्य) को समझ लेना चाहिए-
क़ुरबानी का मतलब
हक़ीक़त में क़ुरबानी का मतलब होता है 'क़रीब' या 'निकट' होना। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन चीज़ों से हम मुहब्बत करते हैं, जिनकी हमारी निगाह में कोई अहमियत है {वे चाहे इस वक़्त हमारी हों या मुस्तक़बिल (भविष्य) में हम उनके मिलने की उम्मीद करते हों, माद्दी (भौतिक) हों या ग़ैर-माद्दी (अभौतिक)} उन्हें हम अल्लाह की रज़ा और ख़ुशी हासिल करने के मुक़ाबले में कभी तरजीह (प्राथमिकता) न दें।
इसी तरह क़ुरबानी ख़ुदा के हुज़ूर क़ुरबत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिआ है। इसीलिए ख़ुदा ने क़ुरबानी को हर उम्मत (समुदाय) के लिए मुतेयन (निश्चित) किया था। क़ुरआन इस बात की तस्दीक़ (पुष्टि) करते हुए कहता है कि- "हम ने हर उम्मत के लिए क़ुरबानी का एक क़ायदा तय कर दिया है ताकि (उसी उम्मत के) लोग उन जानवरों पर ख़ुदा का नाम लें जो उसने उनको अता किये हैं।" (क़ुरआन, सूरा-22 हज, आयत-34)। लिहाज़ा हम देखते हैं कि दुनिया की कोई उम्मत (समुदाय) ऐसी नहीं है कि जिसमें क़ुरबानी का तसव्वुर न पाया जाता हो। मुहम्मद (सल्ल०) से पहले क्योंकि दीन की हक़ीक़ी तस्वीर को बदल दिया गया था इसलिए क़ुरबानी की शक्ल भी बिगड़ कर रह गई थी। यानी लोग क़ुरबानी तो करते थे लेकिन उससे उन्हें न तो कोई रूहानी फ़ैज़ (आध्यात्मिक लाभ) होता और न ही कोई माद्दी फ़ायदा। लेकिन जिस तरह मुहम्मद (सल्ल०) ने पूरे दीन की हक़ीक़ी शक्ल को लोगों के सामने पेश किया उसी तरह क़ुरबानी की हक़ीक़ी शक्ल को भी पेश किया जिससे लोगों को उससे होनेवाले न सिर्फ़ रूहानी फ़ायदे का इल्म हुआ बल्कि माद्दी और दुनियावी (भौतिक) फ़ायदे भी उससे हासिल हो सके।
क़ुरबानी का मक़सद
क़ुरआन में अल्लाह कहता है कि हमने इन्सान को ज़िन्दगी इसलिए अता नहीं की है कि वो जैसे चाहे इसे गुज़ार दे, बल्कि इसलिये अता की है कि वो देखना चाहता है कि इनमें अच्छे अमल करनेवाला कौन है? (क़ुरआन 67:2)। अब जो लोग ख़ुदा के बताए रास्ते पर चलते हैं और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारते हैं वो इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाने में एक-दूसरे की मदद व तआवुन करते हैं और जो लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने के ख़ूगर (आदी) होते हैं वे ख़ुदग़र्ज़ और स्वार्थी हो जाते हैं जिससे ज़मीन पर ज़ुल्म (अत्याचार) और फ़साद (बिगाड़) फैलता है। इस हक़ीक़त के मुताबिक़ ख़ुदा की राह पर चलने वालों (मुस्लिम) और ख़ुदा को न मानकर उसकी नाफ़रमानी करने वालों (काफ़िर) के दरम्यान कभी हमआहँगी (सामंजस्य) पैदा नहीं होती, बल्कि ये काफ़िर (यानी ख़ुदा के नाफ़रमान, ज़मीन पर बिगाड़ पैदा करनेवाले और अशान्ति फैलानेवाले) लोग उन अमन के पैगंबरों (शान्तिदूतों) को सफ़हे-हस्ती से मिटाने की भरपूर कोशिश करने लगते हैं। इस सिलसिले में जो लोग अपने-आपको ख़ुदा का फ़रमाँबरदार और अमन का दाई (यानी मुस्लिम) कहते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि पहले तो उन ज़ालिमों को ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी करने के लिए मुहब्बत और पूरी हमदर्दी के साथ समझाएँ-बुझाएँ और ज़मीन पर सलामती और शान्ति (इस्लाम) क़ायम करने में अपना रोल अदा करने के लिए आमादा और तैयार करें। लेकिन अगर वो इस बात पर आमादा न हों और ज़ुल्म ही करते चले जाएँ तो फिर उनका मुक़ाबला करें और उनको ज़ुल्म और अत्याचार से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें।
क़ुरआन के मुताबिक़ जो लोग ये जिद्दोजुहद (संघर्ष) करेंगे और इस काम के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए आमादा होंगे वो ख़ुदा की रज़ा और उसका क़ुर्ब (निकटता) हासिल करनेवाले लोग होंगे। अब जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि क़ुरबानी का मतलब होता है क़ुर्ब (निकटता) हासिल करना, इसलिए दुनिया भर के मुसलमान ईदुल-अज़हा के मौक़े पर अलामती (Symbolic) तौर पर जानवरों की क़ुरबानी करने को ख़ुदा का क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिआ समझते हैं। इस क़ुरबानी के ज़रिए मुसलमान अपने रब की रज़ा हासिल करने के लिए ये अज़्म करते हैं कि वो ख़ुदा के हुक्म के मुताबिक़ इस दुनिया में इस्लाम यानी शान्ति और सलामती को क़ायम करने के लिए अपना सब कुछ क़ुरबान कर देंगे। यदि ज़रूरत पड़ी तो वे अपने ख़ून की आख़िरी बूँद भी इस रास्ते में बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। क़ुरबानी के इस ख़ास और पाकीज़ा अमल को अंजाम देने से उनका मक़सद समाज में शान्ति और सलामती क़ायम करने के लिए कमरबस्ता होना तो होता ही है, ख़ुदा का क़ुर्ब और रज़ा हासिल करना भी होता है। क्योंकि जो शख़्स जानवर को क़ुरबान करता है वो क़ुरआन के उस हुक्म को ज़रूर-बिलज़रूर ध्यान में रखता है जिसमें अल्लाह कहता है कि "न इन जानवरों का गोश्त हम तक पहुँचता है और न ख़ून, बल्कि सिर्फ़ तुम्हारा तक़वा (परहेज़गारी यानी दिल के अन्दर मौजूद ख़ुदा की सच्ची मुहब्बत और उसकी नाफ़रमानी का ख़ौफ़) पहुँचता है।" (क़ुरआन 22:37)। यानी ख़ुदा देखना ये चाहता है कि जब तुम जानवर को क़ुरबान कर रहे होते हो तो तुम्हारे दिल में हमसे और हमारे दीन से मुहब्बत का जज़्बा कितना है? यही वो जज़्बा था जो बाबा इबराहीम (अलैहि०) के दिल में था। ज़रा ग़ौर कीजिए कि जिस वक़्त बाबा इबराहीम (अलैहि०) ने अपने बेटे इस्माईल (अलैहि०) की गर्दन पर छुरी रख दी थी और अपने जिगर के टुकड़े को क़ुरबान कर देने के लिए तैयार हो गए थे, तो उनके दिल में क्या ख़याल रहा होगा? यही न कि ख़ुदा का हुक्म हो तो मैं अपनी सबसे क़ीमती चीज़ को भी क़ुरबान कर दूँगा!
क्या ख़ुदा हक़ीक़त में बेटे की क़ुरबानी चाहता था?
नहीं! हरगिज़ नहीं! बल्कि वो तो एक आज़माइश और इम्तिहान था जिसमें बाबा इबराहीम खरे उतरे। उन्होंने साबित कर दिया कि वे ख़ुदा की ख़ुशी की ख़ातिर अपनी हर चीज़ क़ुरबान कर देंगे। ये हक़ीक़त में इतनी बड़ी क़ुरबानी थी कि इस क़ुरबानी को रहती दुनिया तक के लिए एक अलामत और प्रतीक (Symbol) बना दिया गया। लिहाज़ा हर साल उसी दिन करोड़ों की तादाद में मुसलमान उस अज़ीम क़ुरबानी की याद ताज़ा करते हैं। बाबा इबराहीम जब बेटे की क़ुरबानी करने जा रहे थे उस वक़्त अल्लाह ने बेटे को बचाकर उस अज़ीम क़ुरबानी को क़बूल कर लिया था। आज हम उसी क़ुरबानी को याद करते हैं लेकिन ये क़ुरबानी ख़ालिस उसी वक़्त होगी जब दिल में जज़्बा वही हो जो बाबा इबराहीम (अलैहि०) के दिल में था कि ख़ुदा का क़ुर्ब और उसकी रज़ा और इस्लाम (यानी समाज में इन्सानी भाईचारा और शान्ति व सलामती) को क़ायम करने के लिए हम हर चीज़ (अपनी सलाहियतें, अपना वक़्त, अपनी दौलत यहाँ तक कि अपने जज़्बात और एहसासात तक) क़ुरबान कर देंगे। ज़ाहिर है कि अब क़ियामत तक किसी ईमानवाले से ये माँग नहीं की जाएगी कि वो अपने बेटे को उस तरह क़ुरबान करे जिस तरह बाबा इबराहीम क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन ख़ुदा की मंशा वही है कि मेरा बन्दा मेरी ख़ुशी और रज़ा के लिए ज़रूरत पड़ने पर अपना सब कुछ क़ुरबान करने के लिए तैयार हो जाए, यही है क़ुरबानी का वो हक़ीक़ी मक़सद जिसे हर मुसलमान ही को नहीं बल्कि तमाम इन्सानों को आज समझने की ज़रूरत है।
क़ुरबानी का तार्किक औचित्य
क़ुर्बानी से सम्बन्धित आक्षेप किए जाते हैं कि हर साल लाखों-करोड़ों बेज़बान जानवर क़त्ल कर दिए जाते हैं और फिर कटाक्ष करते हुए कहा जाता है कि क्या अल्लाह इतना निर्दयी है कि वह बेज़बान पशुओं की जान लेने का आदेश देगा? फिर कहा जाता है कि कहाँ हैं वे जो होली, दिवाली, नवरात्री आदि पर तरह-तरह के कटाक्ष करते हैं? जहाँ तक कटाक्ष का सम्बन्ध है तो इसको किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता धर्म के नाम पर जो आडंबर है उसका विरोध करना आवश्यक है, फिर वो चाहे दिवाली पर छोड़े जाने वाले पटाख़े हों या शबे-बरात पर, धर्म के नाम पर होने वाली ख़राफ़ात चाहे मुहर्रम के नाम पर हो चाहे होली के नाम पर। यदि इन त्योहारों का कोई धार्मिक, सामजिक अथवा आर्थिक औचित्य है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए और जो आडम्बर है उसका विरोध किया जाना चाहिए। यदि होली पर शराब और भाँग पीकर कीचड़ में लथपथ होकर हुड़दंग करने तथा करोड़ों टन लकड़ियों को जलाकर स्वाहा कर देने;... लाखों टन दूध मूर्ती पर चढ़ाने;... दिवाली या शबे-बरात पर अरबों रुपयों को पटाख़ों की शक्ल में फूँक डालने या मुहर्रम और मज़ारों पर चादर चढ़ाने और उर्स इत्यादि पर लाखों रुपयों के ख़र्च कर डालने का कोई भी औचित्य है तो उसे लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। केवल आस्था के नाम पर अंधविश्वास और आडम्बरों को बढ़ावा देना कोई नैतिक एवं तार्किक आधार तो नहीं है। हम यहाँ पर क़ुरबानी के सम्बन्ध में कुछ तार्किक आधार प्रस्तुत कर रहे हैं।
व्यर्थ, अनुचित एवं अन्यायपूर्ण जीव-हत्या से तो सर्वथा बचना ही चाहिए क्योंकि यह मूल-मानव प्रवृत्ति तथा स्वाभाविक दयाभाव के प्रतिकूल है; लेकिन जीवों की हत्या इतिहास के हर चरण में होती रही है क्योंकि बहुआयामी जीवन में यह मानवजाति की आवश्यकता रही है। जीव-हत्या, अपने अनेक रूपों में एक ऐसी वास्तविकता ही नहीं अटल सत्यता है जिससे मानव-इतिहास कभी भी ख़ाली नहीं रहा। इसके कारक सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी। पशुओं, पक्षियों तथा मछलियों आदि की हत्या आहार के लिए भी की जाती रही है, औषधि-निर्माण के लिए भी और उनके शरीर के लगभग सारे अंगों एवं तत्वों से इन्सानों के उपभोग और इस्तेमाल की वस्तुएँ बनाने के लिए भी। बहुत सारे पशुओं, कीड़ों-मकोड़ों, मच्छरों, साँप-बिच्छू आदि की हत्या, तथा शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जीवाणुओं (बैक्टीरिया, germs, वायरस आदि) की हानियों से बचने-बचाने के लिए उनकी हत्या किया जाना सदा से सर्वमान्य और सर्वप्रचलित रहा है। वर्तमान युग में ज्ञान-विज्ञान की प्रगति के व्यापक एवं सार्वभौमिक वातावरण में, औषधि-विज्ञान में शोधकार्य के लिए तथा शल्य-क्रिया-शोध व प्रशिक्षण (Surgical Research and Training) के लिए अनेक पशुओं, पक्षियों, कीड़ों-मकोड़ों, कीटाणुओं, जीवाणुओं आदि की हत्या की जाती रहती है।
ठीक यही स्थिति वनस्पतियों की 'हत्या' की भी है। जानदार पौधों को काटकर अनाज, ग़ल्ला, तरकारी, फल, फूल आदि वस्तुएँ आहार एवं औषधियाँ और अनेक उपभोग की वस्तुएँ तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं; पेड़ों को काटकर (अर्थात् उनकी 'हत्या' करके, क्योंकि उनमें भी जान होती है) उनकी लकड़ी, पत्तों, रेशों (Fibres) जड़ों आदि से बेशुमार कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं। इन सारी 'हत्याओं' में से कोई भी हत्या 'हिंसा', 'निर्दयता', 'क्रूरता' की श्रेणी में आज तक शामिल नहीं की गई, उसे दयाभाव के विरुद्ध एवं प्रतिकूल नहीं माना गया। कुछ नगण्य अपवादों (Negligible exceptions) को छोड़कर (और अपवाद को मानव-समाज में हमेशा पाए जाते रहे हैं) सामान्य रूप से व्यक्ति, समाज, समुदाय या धार्मिक सम्प्रदाय, जाति, क़ौम, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, ईशवादिता आदि किसी भी स्तर पर जीव-हत्या के उपरोक्त रूपों, रीतियों एवं प्रचलनों का खण्डन अथवा विरोध नहीं किया गया। बड़ी-बड़ी धार्मिक विचारधाराओं और जातियों में इस 'जीव-हत्या' के हवाले से ईश्वर के 'दयावान' एवं 'दयाशील' होने पर प्रश्न नहीं उठाए गए, आक्षेप नहीं किए गए, आपत्ति नहीं जताई गई।
क़ुरबानी के माद्दी फ़ायदे (Material benefits)
वैसे तो क़ुरबानी की असल स्प्रिट तक़वा (अल्लाह की नाफ़रमानी (अवज्ञा) से बचते हुए ज़िन्दगी गुज़ारना) है। यानी ये कि जो बन्दा भी क़ुरबानी करे तो क़ुरबानी करते वक़्त वो इस बात का अहद (प्रतिज्ञा) करे कि वो हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक़ उसकी रज़ा के लिए ही करेगा। अल्लाह के हुक्म के सामने वो अपनी महबूब से महबूब चीज़ को भी क़ुरबान कर देगा। यहाँ तक कि अपने जज़्बात व एहसासात तक को क़ुरबान कर देगा। अगर ज़हन व दिमाग़ में वो ख़याल ही न हो तो फिर ज़ाहिर है कि उस क़ुरबानी के माद्दी फ़ायदे जो होंगे वो सब अपनी जगह लेकिन वो हक़ीक़ी और असल रूह हासिल न हो सकेगी। यहाँ पर कुछ लोग ये एतिराज़ करते हैं कि जब क़ुरबानी की स्प्रिट ही ग़ायब है तो क़ुरबानी करना ख़ाह-म-ख़ाह जानवरों का नाहक़ ख़ून बहाना है, इसको बन्द कर देना चाहिए। इस सिलसिले में अर्ज़ है कि किसी अमल की स्प्रिट निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि उस अमल को तर्क ही कर देना चाहिए। स्प्रिट अगर निकल भी गई हो तब भी किसी अमल को दो वजहों से करते रहना चाहिए। पहली बात ये है कि पता नहीं कब इन आमाल के तने-ख़ाकी (बाहरी स्ट्रक्चर) में स्प्रिट पैदा हो जाए और आदमी उस अमल को उसी स्प्रिट के साथ करना शुरू कर दे। दूसरे ये कि कुछ हो या न हो इस अमल के माद्दी (दुनियावी) फ़ायदे इन्सान और उसके समाज को ज़रूर मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं कि क़ुरबानी के माद्दी फ़ायदे क्या हैं?
हमारे देश में मांस बाक़ायदा एक उद्योग है और बहुत बड़ा निर्यात हमारे देश से होता है। हमारे देश की सरकार न केवल मांस के निर्यात बढ़ावा देती है बल्कि नए बूचड़खाने खोलने तथा उनके आधुनिकीकरण के लिए करोड़ों रुपए की सबसिडी भी देती है। यह बात भी दिलचस्प है कि देश के सबसे बड़े चार मांस निर्यातक ग़ैर-मुस्लिम हैं। ईद-उल अज़हा के मौक़े पर लाखों जानवरों की जो क़ुर्बानी होती है उससे देश में अरबों और खरबों रुपयों का चमड़े का व्यवसाय तरक़्क़ी करता है।
मन्दिरों और मठों में श्रद्धा के साथ जो ढोल बजाया जाता है, सेनिकों के वस्त्र एवं देश की रक्षा में काम आने वाले हथियारों के जो कवर और घोड़ों के ज़ीन इत्यादि बनाए जाते हैं वे सब जानवरों की खाल से ही बनते हैं। इनके अतिरिक्त इन्हीं खालों से ऐसी बहुत-सी वस्तुएँ बनाई जाती हैं जिन्हें हम रोज़-मर्रा की ज़िन्दगी में इस्तेमाल करते हैं जैसे:- बेल्ट / बटुआ / पर्स / कंपनी बेग, जेकेट, जूते, चप्पलें इत्यादि
एक और पहलू से देखिए-
क़ुरबानी के जानवर का गोश्त क़ुर्बानी करनेवाले ख़ुद ही नहीं खा जाते बल्कि उसके तीन हिस्से किये जाते हैं जिसमें से एक हिस्सा उन मिलने-जुलनेवालों को दिया जाता हे जिनके घर किसी वजह से क़ुरबानी नहीं होती और एक हिस्सा ग़रीबों और यतीमों को दिया जाता है जिससे उन्हें भरपूर प्रोटिन एवं ओमेगा-3, फ़ैटी एसिड, आयरन, केल्सियम इत्यादि तत्वों से युक्त आहार मिलता है, विश्व स्तर पर ग़रीब लोगों में कुपोषण का स्तर बहुत गिरा हुआ है, इस त्यौहार की बदोलत करोड़ो ग़रीबों को अच्छा और सेहत के लिए अत्यन्त लाभकारी भोजन मिल जाता है। इस ईद पर जिन लाखों जानवरों की क़ुर्बानी की जाती है उनको देश के ग़रीब और किसानों से ख़रीदा जाता है, इस प्रकार उन ग़रीबों को अपने जानवरों की तीन से चार गुना क़ीमत मिलती है, जिससे खरबों रुपयों का बाज़ार में flow होता है, यानी दौलत मालदारों की तिजोरियों से निकल कर ग़रीबों की जेबों में चली जाती है। इसी ईद के अवसर पर हज भी किया जाता है जिससे एयर इंडिया और देश की निजी हज कम्पनियों सहित अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन उद्योग को अरबों-खरबों रुपियों का transaction होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क़ुरबानी का असल मक़सद तो बन्दे के अन्दर क़ुरबानी की स्प्रिट पैदा करना है और इसी को हासिल करने की कोशिश भी की जानी चाहिए, लेकिन क़ुरबानी के भौतिक और दुनियावी फ़ायदे भी कुछ कम नहीं हैं, इसलिए हमें चाहिए कि दिल के ख़ुलूस के साथ हमें क़ुरबानी करनी चाहिए।
क्या मांसाहार मनुष्य को हिंसक बनाता है?
कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों में मांसाहार और क़ुरबानी की मान्यता उनके अन्दर हिंसक प्रवृत्ति (शिद्दत पसन्दी) को जन्म देती है। और एक ही दिन (यानी ईदुल-अज़हा को) करोड़ों की तादाद में जानवरों का ख़ून बहाना इसे धार्मिक मान्यता भी दे देता है। इसकी वास्तविकता पर भी यदि नज़र डालें तो मालूम होगा कि दुनिया में जितने नरसंहार (Mass killings) की घटनाएँ हुई हैं (खाड़ी देशों में थोपे गए युद्ध को छोड़कर), जिनमें अरबों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनमें से किसी में भी मुसलमान शामिल नहीं रहे हैं।
नानकिंग नरसंहार: ये नरसंहार जापान की शाही सेना ने चीन के नानकिंग में किया था। 1937 में हुए इस नरसंहार में 3 लाख लोग मारे गए थे और हज़ारों महिलाओं का रेप हुआ था। ये नरसंहार 6 हफ़्तों तक जारी रहा।
मनीला नरसंहार: दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका से युद्ध में मनीला नागरिकों ने अमेरिका का समर्थन किया जिस पर जापान के लोगों ने लगभग 5 लाख लोग मार दिए।
बॉबी यार नरसंहार: 1941 में जर्मनी की सेना के विरुद्ध यहूदियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैनिकों ने यहूदियों पर क़ब्ज़ा कर लिया और उन्हें बॉबीयार की चट्टान पर ले गए और गोली मारकर लगभग 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
दी होलोकास्ट: एडॉल्फ़ हिटलर और उसके सहयोगियों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को जड़ से मिटाने का फ़ैसला किया। जिसके तहत लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिनमें 15 लाख बच्चे थे।
रवांडा नरसंहार: यह जननरसंहार तुत्सी और हुतु समुदाय के लोगों के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था। इस नरसंहार में 5 से दस लाख लोग मारे गए।
कलिंगा नरसंहार: कलिंग के युद्ध में चकर्वर्ती सम्राट अशोक की सेना ने लगभग डेढ़ लाख लोगों को घरों से बेघर कर दिया था और लगभग एक लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
दो महायुद्धों और अनेक छोटे-छोटे युद्धों में हुई हिंसा में मुसलमानों का शेयर 0 प्रतिशत रहा है। तीन अन्य बड़े युद्धों में मुसलमानों की भागीदारी न की बराबर रही है। राष्ट्रपिता और दो प्रधानमंत्रियों के हत्यारे, मुसलमान नहीं थे। हिंसक प्रवृत्ति में जो लोग दरिन्दों, शैतानों और राक्षसों को भी बहुत पीछे छोड़ गए, हज़ारों इन्सानों को (यहाँ तक कि मासूम बच्चों को भी) ज़िन्दा (लकड़ी की तरह) जलाकर उनके शरीर कोयले में बदल दिए और इस पर ख़ूब आनन्दित तथा मग्न विभोर हुए; गर्भवती स्त्रियों के पेट चीर कर बच्चों को निकाला और उन्हें हवा में उड़ाकर तलवार से दो टुकड़े कर दिए, स्त्री को जलाया, और बच्चे को भाले में गोदकर ऊपर टाँगा और ताण्डव नृत्य किया वे मुसलमान नहीं थे (मुसलमान, मांसाहारी होने के बावजूद इन्सानों का मांस नहीं 'खाते')।
अगर औरतों के साथ ऐसे अत्याचार व अपमान को भी हिंसा के दायरे में लाया जाए जिसकी मिसाल मानवजाति के पूरे विश्व इतिहास में नहीं मिलती तो यह बड़ी अद्भुत, विचित्र अहिंसा है कि (पशु-पक्षियों के प्रति ग़म का तो प्रचार-प्रसार किया जाए, घड़ियाली आँसू बहाए जाएँ, और दूसरी तरफ़) इन्सानों के घरों से औरतों को खींचकर निकाला जाए, बरसरे आम उनसे बलात् कर्म किया जाए, वस्त्रहीन करके सड़कों पर उनका नग्न परेड कराया जाए, घसीटा जाए, उनके परिजनों और जनता के सामने उनका शील लूटा जाए। नंगे परेड की फिल्म बनाई जाए, और गर्व किया जाए! ऐसी मिसालें इस्लाम को सही रूप में मानने वाले मुसलमानों ने कभी भी क़ायम नहीं की हैं। मुहम्मद (सल्ल०) से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त मुसलमानों ने जिन राज्यों को फ़तह किया उनमें शान्ति की स्थापना की। युद्ध के ऐसे नियम और क़ानून बनाए कि रहती दुनिया तक के लोग यदि उनका अनुपालन करें तो हर तरफ़ शान्ति ही शान्ति होगी। प्रोफ़ेट मुहम्मद (सल्ल०) ने युद्ध के मैदान में निहत्थों, धर्मगुरुओं, युद्ध में हिस्सा न लेनेवाले नागरिकों, बच्चों और औरतों पर हाथ तक उठाने को मना किया। तब किस प्रकार कहा जा सकता है कि मांस खानेवाले मुसलमान लोग हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। सच्ची बात ये है कि उनकी इन्सानियत व शराफ़त ने उनको कभी ऐसा करने ही नहीं दिया। ऐसी 'गर्वपूर्ण' मिसालें तो उन पर हिंसा का आरोप लगाने वाले कुछ विशेष 'अहिंसावादियों' और 'देशभक्तों' ने ही अपने ही देश की धरती पर बारम्बार क़ायम की हैं।
जीवों से प्रेम का अर्थ
जीवों से प्रेम का सीधा सा अर्थ यह है कि उनको पाला-पोसा जाए, उनकी देख-रेख की जाए और उनकी नस्लों को बाक़ी और शेष रखने का बन्दोबस्त किया जाए। ख़ुदा ने प्रकृति का सन्तुलन बनाए रखने का ये बन्दोबस्त मनुष्य को ही सौंपा है। इस पहलू से अगर देखा जाए तो हमें मालूम होगा कि इन्सान जिन चीज़ों को खाता है या जो चीज़ें इन्सान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं इन्सान उनको बाक़ी रखने की भी कोशिश करता है। इसके बर-ख़िलाफ़ जिन चीज़ों को वो खाता नहीं है या उसके लिए कम फ़ायदेमंद होती हैं उन्हें न तो वह बाक़ी रखने की कोशिश करता है और न ही उनसे उसे कोई दिलचस्पी होती है। अगर इन्सान शाक-सब्ज़ी अधिक खाता है तो इनकी पैदावार के लिए भी चिन्तित रहता है, जिन शाक-सब्ज़ियों का सेवन मनुष्य नहीं करता है या जो उसके उपयोग में नहीं आती हैं उनके बाक़ी रखने का प्रयास भी क्यों करेगा? इसीलिये उन्हें वो उखाड़ फेंकता है। इसी प्रकार जिन जानवरों के मांस का सेवन जितना अधिक होता है या जो जानवर मनुष्य के किसी काम आते हैं वो जानवर दुनिया में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जिनके मांस का सेवन मनुष्य नहीं करता है या वे मनुष्य के लिए कम उपयोगी हैं वे कम से कमतर होते चले जा रहे हैं यहाँ तक कि बहुत सी प्रजातियाँ तो विलुप्त हो गई हैं और बहुत-सी विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिन जानवरों का सेवन मनुष्य के लिए उपयोगी है यदि उनके सेवन से मनुष्य को ज़बरदस्ती रोक दिया गया तो निश्चित रूप से उनको बाक़ी और शेष रखने में मनुष्य की दिलचस्पी कम से कमतर होती चली जाएगी यहाँ तक कि एक दिन समाप्त ही हो जाएगी।ईदुल-अज़हा और क़ुर्बानी की अहमियत
अक़ल का तक़ाज़ा
अब यदि हम किसी ऐसे जानवर को जीवित और बाक़ी देखना चाहते हैं जिनका सेवन मनुष्य के लिए गुणकारी है तो बुद्धि यह अपेक्षा करती है कि उनके सेवन से मनुष्य को रोका नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो समझ लीजिये कि जानवर की वह प्रजाति एक न एक दिन विलुप्त ही हो जाएगी, जो कि उस प्रजाति के साथ सहानुभूति नहीं बल्कि शत्रुता है।
इस्लाम का पक्ष
इस्लाम में न तो हिंसा अपने अन्दर कुछ हक़ीक़त रखती है और न ही अहिंसा कुछ है। इस्लाम में अस्ल चीज़ है अल्लाह का हुक्म और नबी (सल्ल०) का तरीक़ा। इस्लाम में हिंसा भी है और अहिंसा भी। कब, कहाँ और कैसे हिंसा करनी है और कहाँ हिंसा से दूर रहना है? बन्दों के लिए इसका निर्धारण करना अल्लाह का काम है। जब बन्दा परमेश्वर के इस अधिकार को मान लेता है तभी उसके जीवन में सन्तुलन आता है और तभी कोई व्यक्ति मुस्लिम कहलाने का हक़दार होता है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि यदि किसी ने दोस्ती की अल्लाह के लिए, दुश्मनी की तो अल्लाह के लिए, किसी को दिया तो अल्लाह के लिए और किसी से कुछ रोका तो अल्लाह के लिए तभी उसका ईमान मुकम्मल होता है। जिन लोगों ने परमेश्वर के इस अधिकार को नहीं माना और अपनी मर्ज़ी से हिंसा की, उन्होंने धरती को रक्तरंजित कर तबाह कर डाला और जिन लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया में केवल अहिंसा का उपदेश दिया उन्होंने भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे उपदेशकों ने दूध, दही, शहद, अंजीर, अचार और लहसुन-प्याज़ जैसी गुणकारी चीज़ों तक के सेवन से रोक दिया। याद रखना चाहिये कि क़ुरबानी से हिंसा और अहिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं है। क़ुर्बानी करने वाला और हलाल मांस खाने वाला भी दीन-दुखियों की सेवा में लगा देखा जा सकता है। इसके विपरीत बहुत-से शाकाहारियों को इंसानों की लाशों पर ताण्डव करते हुए देखा गया है। ऐसे शाकाहारी लोग तो निहत्ते और बेगुनाह आदमी को मारते हुए भीड़ की शक्ल में आए दिन देखे जा सकते हैं। ऐसे बहुत से पंथ हैं जिनमें कोई एक चीज़ खाता है और दूसरा उस चीज़ को खाना पाप समझता है। स्वयं शाकाहारियों में भी आपस में इस विषय पर सहमति नहीं है। कुछ शाकाहारी तो ऐसे हैं जो दूध, दही और शहद आदि खाते हैं परन्तु कुछ दूसरे ऐसे भी हैं जो इन्हें खाना पाप और अमानवीयता मानते हैं। ऐसे में या तो हरेक आदमी अपने-अपने पैमाने पर पूरा उतरने का प्रयास करेगा या फिर सबको मिलकर सबके लिए किसी एक पैमाने को स्टैंडर्ड पैमाना मान लेना चाहिए, जिस पर हरेक आदमी के कर्म को परखा जा सके कि उसने नेक काम किया है या बद; पुण्य किया है या पाप? और वह पैमाना ईश्वरीय आदेश से बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। जब तक ईश्वर प्रदत्त इस एक पैमाने को सबके लिए स्टैंडर्ड पैमाना न मान लिया जाए तब तक अनेक पैमाने बनते रहेंगे जिनमें परस्पर विरोध का पाया जाना स्वाभाविक ही है। ऐसे में या तो ख़ामोश रहा जाए या ईश्वर प्रदत्त पैमाने को स्वीकार कर पूरी मानवता को एक ही रंग में रंगने का प्रयास किया जाए। इसलिए ईदुल-अज़हा केवल खाने-पीने का मसला नहीं है बल्कि इसके साथ और भी बहुत-से ऐसे बिंदु जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रहित में भी उपयोगी हैं और मानवहित में भी और स्वयं उन जानवरों के हित में भी जिनकी क़ुरबानी की जाती है।
ईदे-क़ुर्बाँ का हासिल क्या?
मुसलमान ईदे-क़ुर्बां को मनाने के लिए कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। जानवरों की ख़रीदारी होती है, अच्छे से अच्छा जानवर तलाश किया जाता है, छुरियों की धार तेज़ की जाती है। ये सब काम सही हो सकते हैं। लेकिन क्या हम ईमान की धार को भी तेज़ कर पाते हैं कि अपनी अना को अपने अल्लाह के लिए ज़बह कर सकें? क्या हम तक़वा को धार लगा पाते हैं? कि दुनिया की मुहब्बत को अल्लाह की मुहब्बत की ख़ातिर क़ुर्बान सकें। क्या हम अपने ईमान को भी चाँड सके कि अपने नफ़्स के देव को नहर (ज़बह) कर सकें। जिस तरह हमने जानवरों को बे-ऐब तलाश किया था उसी तरह क्या हमने अपने दिल के अन्दर के ऐबों को भी तलाश करने की कोशिश की? हज़रत इबराहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को तो ज़िन्दा कर दिया, लेकिन क्या हज़रत इबराहीम का अल्लाह के लिए क़ुरबानी का वो जज़्बा भी ज़िन्दा कर पाए? क्या उस वफ़ा को भी याद कर पाए जिसका उन्होंने अल्लाह के लिये हक़ अदा कर दिया था? ये कैसी अजीब बात है कि क़ुरबानी का जानवर तो हो बे-ऐब, लेकिन क़ुरबानी करने वाले इन्सान के दिल में शिर्क और निफ़ाक़, हसद और अहंकार, एहसान फ़रामोशी और कमज़र्फ़ी, बुज़दिली और तंगदिली, निफ़ाक़, फ़िस्क़ और शिर्के-ख़फ़ी जैसे हज़ार तरह के ऐब पाए जाते हों। इन्हीं सब तरह के रोगों को दिलों से निकालने के लिए अल्लाह ने क़ुरबानी को एक symbol के तौर पर वाजिब किया था, और सिखाया था कि इस symbolic क़ुरबानी को करते वक़्त तुम ये अहद किया करो कि- मैंने चारों तरफ़ से काटकर अपना रुख़ अपने रब की तरफ़ कर लिया है, और ये कि- मेरी नमाज़, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना और मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है।
हाय अफ़सोस कि गोश्त तो हम खाते हैं दोस्तो; और ग़रीबों को भी ख़ूब खिलाते हैं लेकिन उस अहद को बिलकुल भूल जाते हैं जो हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने अपने रब से किया था जब उनके रब ने उनसे कहा कि तुम मेरे फ़रमाँबरदार हो हो जाओ तो उन्होंने फ़ौरन अहद किया कि मैं तो रब्बुल-आलमीन का फ़रमाँबरदार हो गया। याद रखना दोस्तो, अल्लाह का साफ़ ऐलान है कि हम तक तुम्हारे गोश्त और ख़ून नहीं पहुँचते, बल्कि दिल की वो कैफ़ियत (तक़वा) पहुँचती है जो क़ुरबानी के वक़्त तुम्हारे अन्दर होती है। अगर दिल की कैफ़ियत महज़ गोश्त खाने और नमूद व नुमाइश की है तो फिर जान लीजिये कि बज़ाहिर भले ही तुमने गोश्त की तक़सीम नाप-तौलकर बड़ी बारीकी से की हो, जानवर को क़ुर्बान करते वक़्त क़ुरआनी आयात और दुआएँ भी ठीक-ठीक पढ़ी हों, क़ुरबानी से पहले छुरी की धार भी ख़ूब तेज़ कर ली हो, जानवर का रुख़ भी दुरुस्त कर लिया हो लेकिन अल्लाह से किये हुए वादे तुमको याद नहीं हैं, अल्लाह से वफ़ादारी का अहद तुम भुला चुके हो तो तुम इन बे ज़बान जानवरों का नाहक़ ख़ून बहा रहे हो। और सड़कों और रास्तों पर गन्दगियाँ फैलाकर न सिर्फ़ इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हो बल्कि लोगों को बीमार करने का गुनाह भी अपने सिर ले रहे हो। दोस्तो जब हम ये सब काम कर ही रहे हैं तो आइए अपने जज़्बे को भी दुरुस्त करने का अहद करें।