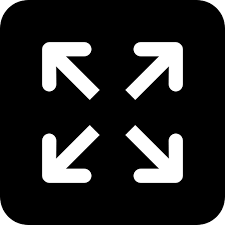- Home
- /
- Top Stories
- /
- नफरत के शिकार रहे लालू...

शकील अख्तर
जिस चीज से आपको सबसे कष्ट हो क्या वह चीज आप दूसरे के लिए कर सकते हैं? सामान्यत: नहीं। सभ्यता और शिष्टता में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास के नाम को बिगाड़कर उनका अपमान करने की कोशिश की वह भारी आश्चर्यजनक और दुखद है। लालू जी का सबसे ज्यादा अपमान उनके नाम को बिगड़कर ही करने की कोशिश की गई है। कई नेताओं के अलावा टीवी एंकर और पत्रकार भी उनके नाम को बिगाड़कर उसका मजा लेने की कोशिश करते हुए देखे गए हैं। सभ्य समाज में जो और चीजें रंग, जाति, धर्म, लिंग, कपड़े मजाक का विषय नहीं हो सकते वैसे ही नाम, शारिरिक बनावट, भाषा, लहजा भी नहीं। हालांकि हमारे यहां शिष्टाचार का यह परिदृश्य अभी बहुत दूर है। मगर अफसोस की इस पर काम भी, बात भी नहीं होती है। राही मासूम रजा ने अपने मशहूर उपन्यास नीम का पेड़ में इस पर बहुत गहराई से लिखा है कि किस तरह नामों को बिगाड़ा जाता है और उसे अपमान का जरिया बनाया जाता है। नाम किस तरह सामाजिक स्थिति के अनुरूप छोटे, गंदे, उपहासजनक बना दिए जाते हैं।
इन्हीं सबसे निपटने का सिद्दांत सामाजिक न्याय था। लालू जी इसके बहुत बड़े चैम्पियन रहे। बिहार में राजद के लोग कहते हैं कि लालू जी ने क्या दिया? लालू जी पिछड़े को सम्मान दिया। वह आत्मविश्वास से चाहे जहां खड़ा हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। मगर लालू जी सम्मान देने की अपनी इस बात को विस्तार नहीं दे पाए। मानते हैं कि सिद्दांत का खुद पर लागू करना बहुत मुश्किल होता है। गोस्वामी तुलसीदास के "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" से लेकर इकाबाल के
" इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों से मोह लेता है
गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका !"
शेर में यह बात कही गई है। मगर उन लोगों को तो इसे समझना और अमल में लाने की कोशिश करना चाहिए जिनके लिए यह सिद्धांत बहुत महत्व रखता है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत ने ही लालू, मुलायम सिंह यादव, मायावती, को सत्ता दिलाई। लेकिन उसके बाद ये भी सामंती मानसिकता के शिकार हो गए। खुद को ऊंचा समझना एक बार चल जाएगा। अगर वह हवा में हो तो। मगर समस्या यह है कि जमीन पर खुद को उंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा करना पड़ता है। यही सामंतवाद है। इसके कई विकृत रुप लालू और मायावती ने दिखाए हैं। यहां कोई उदाहरण नहीं दे रहे या विस्तार से नहीं लिख रहे क्योंकि उन बातों को बढ़ाने में हमारा विश्वास नहीं है। हालांकि अन्य ट्रोलों की तरह दलित और पिछड़े नेताओं के समर्थक भी एकदम से आपा खोकर उसी तरह गंदे स्तर पर आ जाते हैं। मगर फिर भी हमारा मानना है कि उन्हें जब तक हो सके थोड़ा मार्जन देना चाहिए। उनके समाज के नेताओं के बढ़ने की शुरूआत नई है और ऐसे में उनके अन्तरविरोध का सामने आना समर्थकों को बहुत विचलित कर जाता है। इसे समझना चाहिए।
मगर खुद नेताओं को अपने समर्थकों से उपर उठकर इस बात को समझाना चाहिए कि नाम, जाति को लेकर किए गए व्यंग्य आत्मघाती होते हैं। बैक फायर करते हैं। सामाजिक न्याय के नेताओं में लालू जी का नाम सबसे बड़ा है। इसलिए भाजपा और आरएसएस ने सबसे ज्यादा हमले उन्हीं पर किए। उन्हें यह बात समझना चाहिए कि हमले उनके विचारों के कारण थे। और अगर अपने ये विचार वे डाय्लूट ( ताक पर रखना) कर देंगे तो फिर ओबीसी के लिए वे और दूसरे यथास्थितिवादी एक समान ही हो जाएंगे। बिहार में ही रामविलास पासवान और उसके बाद चिराग पासवान से दलितों का छिटकना उन्होंने खुद देखा है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में होता लग रहा है। वहां मायावती के भाजपा के साथ होते दिखने के कारण पहली बार ऐसा हो सकता है कि दलित उनका साथ छोड़ जाएं। दलितों को अगर भाजपा के साथ ही जाना होगा तो वे वाया मायवती क्यों जाएं? लोकसभा चुनावों में जैसे गए थे सीधे खुद ही भाजपा के साथ चले जाएंगे। या कहीं और जाना होगा तो वहां जाएंगे। मायवती के साथ होने का मतलब कांशीराम और उस विचार के साथ खड़े होना है जो डा. आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले से शुरू हुआ था। बड़ा विचार। समानता का। लेकिन अगर मायवती इसी के खिलाफ चली जाती हैं तो क्या दलित उनके साथ रहेंगे?
दलितों को अभी लंबी दूरी तय करना है। पिछले 74 साल में उन्होंने सबसे ज्यादा तरक्की की। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर क्षेत्र में। मगर पीछे सदियों से धकेला जाता रहा था तो आगे आने, बराबर आने के लिए भी और समय चाहिए। मगर क्या इस और आगे आने के लिए मायावती या दूसरे दलित नेताओं का नेतृत्व अब प्रभावी बचा है? रामविलास पासवान एक बड़े उदाहरण हैं। अपने समाज से उन्होंने सब कुछ पाया। बड़े दलित नेता के तौर पर जाने गए। जब कांशीराम जी थे और मायावती व्यवस्था के खिलाफ वाकई लड़ रही थीं तब हर चुनाव में पासवान खुद को दलित नेता बताकर यूपी में वोट बांटने आ जाते थे। मीडिया में पासवान ने एक बहुत ही मजबूत गेंग बना रखी थी। वह पासवान को ऐसा चढ़ाती थी कि लगता था कि दलितों का उनसे बड़ा उद्धारक आज तक कोई हुआ ही नहीं। पासवान देश के वह एकमात्र नेता थे जो अपने निजी खर्चे पर पत्रकारों की एक बड़ी टीम को अमेरिका घुमा कर लाए थे। लेकिन उनके न रहने पर कोई विचार नहीं रहा। केवल आपस में लड़ते हुए उनका बेटा और भाई रह गए। और दलितों के पास छले होने का एक दुःखी अहसास।
नेतृत्व काम न कर सके यह क्षम्य है। मगर खुद बन जाए और जनता वैसी ही रह जाए तो यह सोचने की बात है। पासवान और मायवती खुद समर्थ और सम्पन्न होते चले गए। इतने कि दोनों को उस वैभव को बचाने के लिए सत्तारुढ़ भाजपा के साथ जाना पड़ा। और वही आखिरी नियति हो गई।
लालू जी संघर्ष किया। जेल गए। डरे नहीं। वाकई बहुत साहस की बात है। कांग्रेस से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर विरोध करने के लिए वह जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह नफरत से उपजी है। उसी ऊंच नीच, भेदभाव की भावना से उपजी नफरत जिसका शिकार वे खुद होते रहे हैं। भक्तचरण दास दलित हैं। उनके काम, तरीके, विचार किसी पर भी लालू जी टिप्पणी कर सकते हैं। मगर हिकारत से उनका नाम लेना यह बताता है कि वंचित, शोषित तबके में भी विचार के स्तर पर सामाजिक न्याय का पूरा कान्सेप्ट क्लीयर नहीं है। कई जाले वहां लगे हुए हैं। अम्बेडकरवाद, पिछड़ा उत्थान का नारा तेज हो रहा है। मगर प्रगतिशीलता से उसका द्वंद कराया जा रहा है। जबकि प्रगतिशीलता हमेशा से उसे मजबूत करने वाली ताकत रही है। बिहार में भाजपा और नीतीश की बड़ी ताकत से तेजस्वी कांग्रेस और लेफ्ट के सहयोग से लड़ पाए। इन दोनों के साथ खड़े होने से ही जंगल राज के प्रचार की हवा निकल गई। ऐसे ही यूपी में बीस साल पहले जब मुलायम ने लेफ्ट से समझौता किया था तभी उनकी विश्वसनीयता बनी थी। जीते थे। उस समय 2002 में भाजपा और मायवती ने मुलायम की छवि बहुत खराब कर रखी थी। लेकिन फिर अमर सिंह के प्रभाव में मुलायम ने 2007 में लेफ्ट के साथ धोखा किया। हार गए। उसी समय मायावती ने यह प्रसिद्ध वाक्य कहा था कि मरे को क्या मारना! उसके बाद ही मुलायम कभी वापस सत्ता में नहीं आ पाए। पासवान की तरह ही परिवार भाई और बेटे में बंट गया।
यूपी, बिहार में कांग्रेस कमजोर है। लेफ्ट और ज्यादा। मगर इनका साथ आना एक चमक देता है। विश्वसनीयता। जातिवादी पार्टी से हटकर एक सबकी पार्टी का आश्वस्तकारी संदेश!