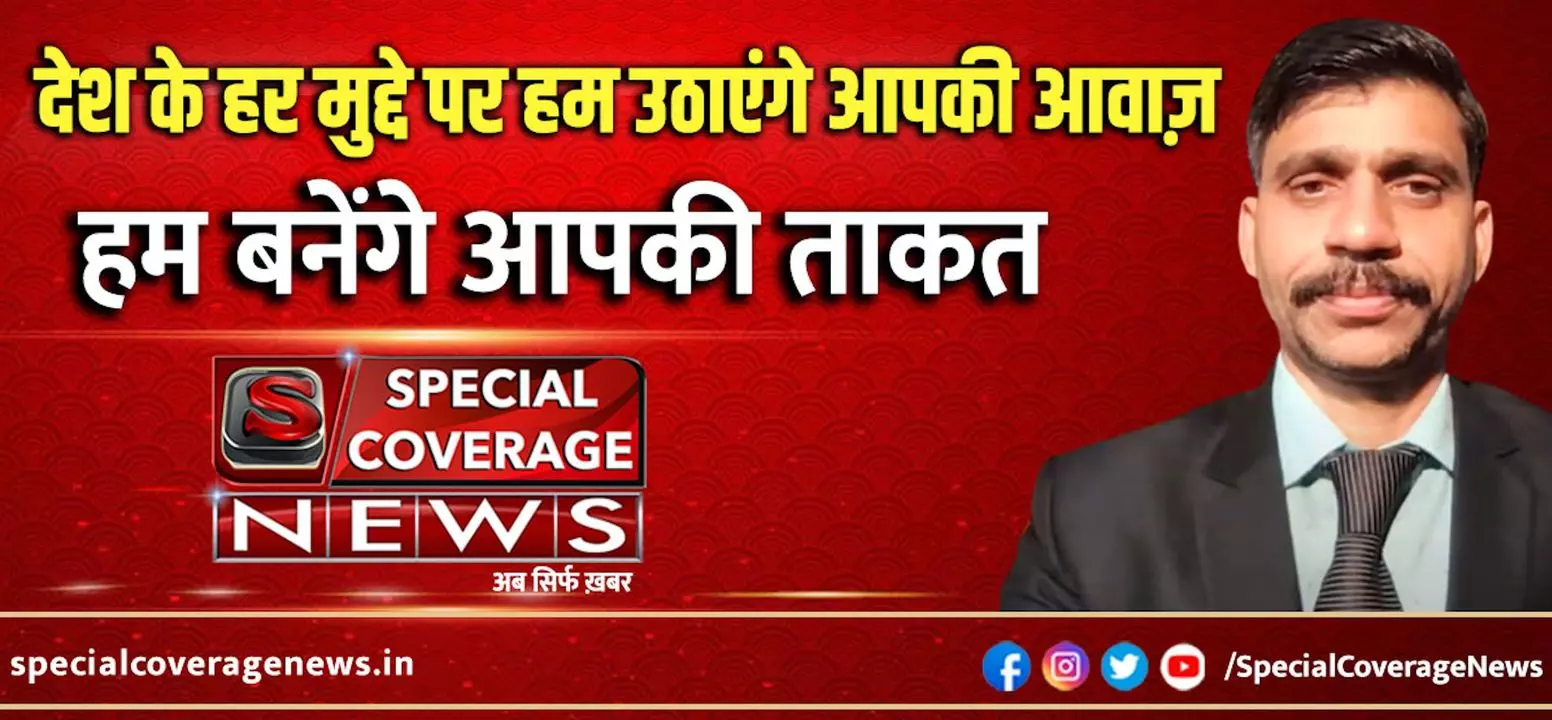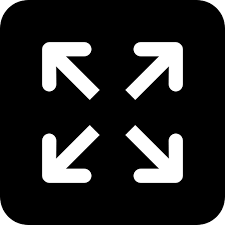- Home
- /
- Top Stories
- /
- यूपी के चुनावी-नतीजे...
यूपी के चुनावी-नतीजे का राजनीतिक अर्थ क्या? वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की कलम से

उर्मिलेश
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बारे में तरह-तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं। यह महत्वपूर्ण चुनाव था, जिसमें कोई सत्ताधारी पार्टी वर्षों के अंतराल के बाद दोबारा सत्ता में आई है। इसका क्या मतलब है? क्या निवर्तमान सरकार वाकई बहुत लोकप्रिय थी? बीते पांच साल के घटनाक्रम, शासकीय कामकाज के ब्यौरे, मानव विकास सूचकांक में यूपी की दयनीय स्थिति, राज्य में नागरिकों के दमन-उत्पीड़न के मामले, महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार के सरकारी-आंकड़े (राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज शिकायतें), शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति-व्यक्ति आय के अधिकृत आंकड़े को देखते हुए राज्य की भाजपा सरकार के शासकीय मॉडल या उसके कामकाज को न तो अच्छा कहा जा सकता है और न संतोषजनक।
फिर भी मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया। देश-विदेश में रहने वाले अनेक राजनीतिक विश्लेषकों ने यूपी में भाजपा की जीत को समाज और सियासत के 'हिन्दुत्वीकरण' का नतीजा कहा है। कुछ विपक्षी राजनीतिज्ञों ने इसके पीछे ईवीएम की कथित अदला-बदली से लेकर चुनाव अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत से की गयी धांधली को बड़ा कारण माना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खासतौर पर ऐसे आरोप लगाये हैं। उनके मुकाबले कुछ मद्धिम स्वर में अखिलेश ने भी चुनावी धांधली के कुछ प्रसंगों के हवाले गड़बड़ी की बात कही है।
ममता बनर्जी ने इस चुनाव में अखिलेश यादव की अगुवाई वाले सपा-गठबंधन के पक्ष में चुनाव-प्रचार भी किया था। बहरहाल, हमारे पास बड़े पैमाने पर ईवीएम बदले जाने या उसमें कोई गड़बड़ी करने जैसे ठोस साक्ष्य नहीं हैं, इसलिए ऐसे आरोपों को इस आलेख में विश्लेषित करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। भाजपा की जीत के सिर्फ सामाजिक-राजनीतिक कारणों की हम यहां पड़ताल करेंगे।
'हिन्दुत्व-लहर' के अलावा 'लाभार्थी-मतदाताओं' के भाजपा के समर्थन में खामोश रहकर वोट देने को भी जीत का एक बड़ा कारण माना गया है। बारी-बारी से हम ऐसे तमाम कारणों और कारकों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, क्या भाजपा की जीत सिर्फ 'हिन्दुत्व-लहर' के चलते हुई है? इस बार 403 सदस्यीय सदन में भाजपा को 255 सीटें मिलीं जो पिछले चुनाव से 57 कम हैं। वोट प्रतिशत में मामूली इजाफा हुआ, जबकि उसके मुख्य प्रतिद्वन्द्वी समाजवादी पार्टी को इस बार सीट और वोट प्रतिशत, दोनों में भारी बढ़ोत्तरी मिली। पर सत्ता की लड़ाई में भाजपा ने उसे काफी पीछे छोड़ दिया। यह सब क्यों और कैसे हुआ? अगर यह 'हिन्दुत्वीकरण की जीत' है तो भाजपा की सीटें 2017 के मुकाबले कम कैसे हो गयीं। ध्रुवीकरण मे सीटें बढ़ती हैं, घटने के उदाहरण कम मिलते हैं।
देश के एक जाने-माने लिबरल सिद्धांतकार ने कहा कि यूपी में जबर्दस्त 'हिन्दू-ध्रुवीकरण' करके भाजपा ने चुनाव जीता। अगर ऐसा होता तो सन् 2017 में 24 के मुकाबले इस चुनाव में 34 मुस्लिम विधायक कैसे चुने गये? ऐसे चुनाव क्षेत्रों से भी कुछ मुस्लिम विधायक जीते हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं के 10 से 20 फीसदी है। कुछ सीटों पर 30 फीसदी या उससे कुछ ऊपर भी है। भाजपा ने एक भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया था। जीते हुए सारे विधायक समाजवादी पार्टी-गठबंधन के हैं। सच ये है कि नवनिर्वाचित मुस्लिम विधायकों में ज्यादातर हिन्दू आबादी के समर्थन के बगैर नहीं जीत सकते थे।
इस चुनाव को 'हिन्दुत्व लहर' का चुनाव बताने का दावा जमीनी तथ्यों से भी मेल नहीं खाता। 'हिन्दुत्व' जैसी राजनीतिक विचारधारा के पक्के समर्थक या पैरोकार यूपी के समाज में आज भी बहुत सीमित हैं। उच्चवर्णीय हिन्दू वैश्य और कायस्थों का बड़ा हिस्सा इसका प्रमुख पैरोकार है। यूपी और समूचे हिन्दी भाषी क्षेत्र में मीडिया का बड़ा हिस्सा भी इसमें शामिल है। इन सबकी पसंद आज भाजपा है। अक्सर य़े हिस्से कोशिश करते हैं कि आम लोग 'हिन्दुत्व' जैसे राजनीतिक विचार को हिन्दू धर्म का पर्याय समझ लें पर समाज के व्यापक हिस्से में आज तक ऐसा नहीं हो सका है। तमाम कोशिशों के बावजूद समाज के ज्यादातर हिस्से में सामाजिक रिश्ते टूटे नहीं हैं।
कल्पना कीजिये, निकट-भविष्य में कोई सुसंगत लोकतांत्रिक-सेक्युलर सरकार आ जाये तो आज के माहौल की सांप्रदायिक-भयावहता अपने-आप कम हो जायेगी। राज्य की अस्सी फीसदी से ज्यादा आबादी के लिए रोजमर्रे के मसले सबसे अहम् हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और बेरोजगारी के मामले में यूपी की हालत बहुत खराब है। राजनीतिक पार्टियां इन्हीं आम लोगों को अपने-अपने तईं प्रभावित करके चुनाव जीतने की कोशिश करती रहती हैं। भाजपा इन्हें प्रभावित करने के लिए 'हिन्दुत्व' के राजनीतिक विचारों का इस्तेमाल करती है। इस चुनाव में भी उसने इसकी हर संभव कोशिश की। पर ऐसा कोई प्रामाणिक और वैज्ञानिक आकलन या सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित हो कि पर आम मतदाताओं ने हिन्दुत्व-विचार के आधार पर मतदान किया। ऐसे दावे सिर्फ भाजपा के कुछ नेताओं के बयानों और मीडिया के एक हिस्से की खबरों और विश्लेषणों में ही मिल रहे हैं।
सच ये है कि पश्चिम से पूरब तक, अति-पिछड़ी और दलित जातियों के असंख्य लोगों ने मुफ्त अनाज योजना और पीएम-किसान निधि जैसी सीधी आर्थिक मदद को मोदी-योगी सरकारों की निजी 'मेहरबानी' मानकर उनकी पार्टी को मतदान किया। लोगों के ऐसे भावों को भाजपा ने 'नमक का वास्ता' देकर प्रचारित किया। लोगों से य़ह तक कहा कि वे वोट देते समय 'नमकहरामी' न करें। पिछले दिनों मैंने ऐसे अनेक वीडियो देखे, जिनमें लोग महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना-दौर में योगी सरकार की भयानक नाकामी और छुट्टा पशुओं द्वारा फसलों की बर्बादी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सत्ताधारी दल से अपनी गहरी नाराजगी के बावजूद कहते सुने गये कि उन्होंने मुफ्त अनाज योजना और 6 हजार सालाना आर्थिक मदद के चलते सत्ताधारी दल को वोट किया।
विपक्ष की तरफ से ऐसे 'लाभार्थियों' के बीच सरकारी योजनाओं को लेकर कोई दूसरा विमर्श नहीं पहुंचा। सक्रिय, समझदार और गतिशील विपक्ष के अभाव के चलते ऐसा हुआ। अगर विपक्षी खेमा सक्रिय और समझदार होता तो लाभार्थी-मसले को बिल्कुल अलग आयाम दे सकता था। पर यूपी में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, दोनों के शीर्ष नेता पौने पांच साल अपने-अपने बंगलों से सत्ता-पक्ष पर सिर्फ 'ट्विटर-वार' कर रहे थे। उऩके ट्विटर-वार को तो नोएडा के टीवीपुरम् से 'एंकर' ही निष्प्रभावी कर दिया करते थे। दोनों दलों का संगठन चरमरा गया था। समाजवादी पार्टी का तो और भी बुरा हाल था। बसपा सुप्रीमो लगातार सतर्क रहीं कि केंद्र और राज्य के सत्ताधारी उनसे नाराज न हों। वह विपक्ष की भूमिका में ही नहीं रहीं। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी को बेहद कमजोर कर दिया था।
सपा नेतृत्व ने चुनाव की घोषणा से महज तीन-चार महीने पहले गत वर्ष अक्तूबर-नवम्बर में जनता के मुद्दों और शासन के जन-विरोधी रवैये पर सवाल उठाना शुरू किय़ा। इससे पहले अखिलेश यादव भी ट्विटर तक सीमित थे। अखिलेश ने पिछले वर्ष नवम्बर महीने में गाजीपुर से लखनऊ की बहुचर्चित विजय रथयात्रा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की जबकि उनके सामने एक ऐसा सत्ताधारी दल था, जिसके पास सिर्फ सत्ता की ही ताकत नहीं थी, आरएसएस की छतरी के नीचे साल भर लोगों के मानस को प्रभावित करने वाले दर्जनों संगठनों का विशाल नेटवर्क भी था।
अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य
योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और पिछड़े वर्ग के अन्य प्रमुख नेताओं ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में जब सरकार और पार्टी से इस्तीफा दिया तो सरकारी नीतियों और फैसलों से नाराज बहुजन में बड़ी एकता की संभावना प्रबल दिखी। लेकिन यूपी जैसे बड़े प्रदेश में किसी सुव्यवस्थित और सुसंगत सोच आधारित विपक्षी संगठन के बगैर वह बड़ी एकता नहीं कायम हो सकी। आरएसएस-भाजपा ने वर्षों से कुशवाहा-कुर्मी-गूजर-लोध जैसी पिछड़ी जातियों में जितना प्रभाव-विस्तार कर रखा था, उसे महज एक महीने में पलटना कैसे संभव होता?
इसके लिए सिर्फ कुछ नेता-विधायकों का दल-बदल पर्याप्त नहीं था। यूपी में न तो केरल और तमिलनाडु जैसी संगठित गैर-भाजपा पार्टियां-माकपा या डीएमके थीं और न ही ममता बनर्जी जैसा कोई 'निडर राजनीतिक योद्धा' था। विपक्षी दलों का बड़ा हिस्सा शीर्ष सत्ताधारी नेताओं पर प्रतिकूल टिप्पणी करने से भी बचता था। इसके पीछे केंद्रीय एजेंसियों का डर बताया जाता है। प्रतिपक्ष के खेमे की सबसे बड़ी पार्टी-सपा के साथ एक और समस्या थी। पार्टी के नाम में तो 'समाजवादी' लगा है पर वह समता और सामाजिक न्याय के उसूलों को लेकर कभी मुखर नहीं रही। पहली बार इस चुनाव में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण और जाति-आधारित जनगणना जैसे मुद्दों का अपने एक शुरुआती भाषण में जिक्र किया। लेकिन '22 में 22 संकल्प' शीर्षक पार्टी मैनिफेस्टो में इनका उल्लेख तक नहीं किया।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने या उनका गैर-जरूरी विनिवेश करने की सरकारी नीति की मुखालफत और निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसी ओबीसी-दलित समुदाय की लोकप्रिय मांगों की भी मैनिफेस्टो में कोई चर्चा नहीं। इससे सपा के राजनीतिक नेतृत्व के मिजाज और विचार का अंदाजा लगाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के बुल्ड़ोजर जैसे विध्वंसक और डरावने प्रतीक के विरुद्ध रोजगार, महंगाई, आरक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में ज्यादा खर्च आदि के सवालों को आगे करके अखिलेश सृजनात्मक और समावेशी प्रतीक गढ़ सकते थे। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समझना कठिन है कि वह जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे या हारने के लिए?
इसे परिस्थितियों का संयोग कहें या कोई खास योजना, यूपी में इस बार का चुनाव दो-ध्रुवीय हो गया। मुख्य विपक्षी के रूप में सपा ही उभरी। अचरज की बात कि अखिलेश ने यह जानते हुए भी कि यूपी में मायावती जी और उनकी बसपा अब दलितों के बीच अपना आकर्षण खो रही है और इस बार दलित-वोटों का भारी विभाजन होने जा रहा है, उन्होंने दलित-मतदाताओं को अपने साथ लाने की कोई ठोस कोशिश नहीं की। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांशीराम के सहयोगी रहे दद्दू प्रसाद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को अपने साथ जोड़ने की बजाय उन्हें अलग ही रखा। स्वयं अपनी पार्टी के दर्जन भर से ज्यादा बड़े इलाकाई नेताओं को चुनाव प्रचार में नहीं उतारा।
हर जगह अखिलेश और सिर्फ अखिलेश ही दिखे। पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी ने भी वही गलतियां कीं। किसान आंदोलन के प्रभाव के इलाके में भी गठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पूर्वांचल के गोरखपुर, कुशीनगर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया और महराजगंज जैसे कई जिलों में सपा के बुरे प्रदर्शन के पीछे किसी 'हिन्दुत्व लहर' कारण नहीं थी, उसकी सांगठनिक कमजोरी और अनुपयुक्त प्रत्याशियों के चयन के चलते ऐसा हुआ। इसके अलावा भाजपा ने सत्ता में होने और चुनाव आयोग के बेहद कमजोर होने के हर संभव फायदे उठाये। चुनावी धांधली हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। पर विपक्ष ने उसका भी प्रामाणिक ढंग से पर्दाफाश नहीं किया। बिल्कुल आखिर में वाराणसी, बरेली और सोनभद्र जैसे कुछ जिलों के मामलों को अखिलेश यादव ने सामने लाया। चुनाव आयोग ने उन मामलों में कुछ स्थानीय अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया या चुनाव ड्यूटी से हटा दिया। लेकिन चुनाव-धांधली का कोई पर्दाफाश सामने नहीं आया।
ऐसे में महज आरोपों के आधार पर विपक्ष अपनी हार के लिए चुनावी-धांधली का बहाना नहीं खोज सकता है। मजे की बात है कि चुनावी-धांधली के लिए रास्ता बनाने वाले कतिपय फैसलों को किसी विपक्षी दल ने चुनौती तक नहीं दी। चुनाव से काफी पहले जब निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट का दायरा बढ़ाने का नियम बनाने के लिए सर्वदलीय संपर्क किया तो सपा, बसपा या कांग्रेस की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। बाद में इन दलों ने पोस्टल बैलेट से हो रही धांधली का रोना शुरू किया। बसपा और कांग्रेस, जैसी देश की बड़ी पार्टियों के लिए यूपी चुनाव न सिर्फ निराशाजनक अपितु सफाये का सिग्नल साबित हुआ। देश की सबसे पुरानी पार्टी-कांग्रेस को विधानसभा की कुल 403 में सिर्फ 2 और प्रदेश में चार-चार बार सरकार बनाने वाली बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली। दोनों की भयावह विफलता की अलग-अलग वजह है।
सत्ताधारी भाजपा की जीत और मुख्य विपक्षी सपा की हार के लिए एक नहीं, कई कारण नजर आते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख कारणों की हमने ऊपर चर्चा की है। राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कारण है-मुख्य विपक्षी दल की अपनी नाकामियां। मजबूत संगठन का न होना, विचारों की अस्पष्टता और नेतृत्व की निष्क्रियता!
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राज्यसभा चैनल के कार्यकारी प्रमुख रहे हैं। आजकल दिल्ली में रहते हैं।)
साभार जनचौक