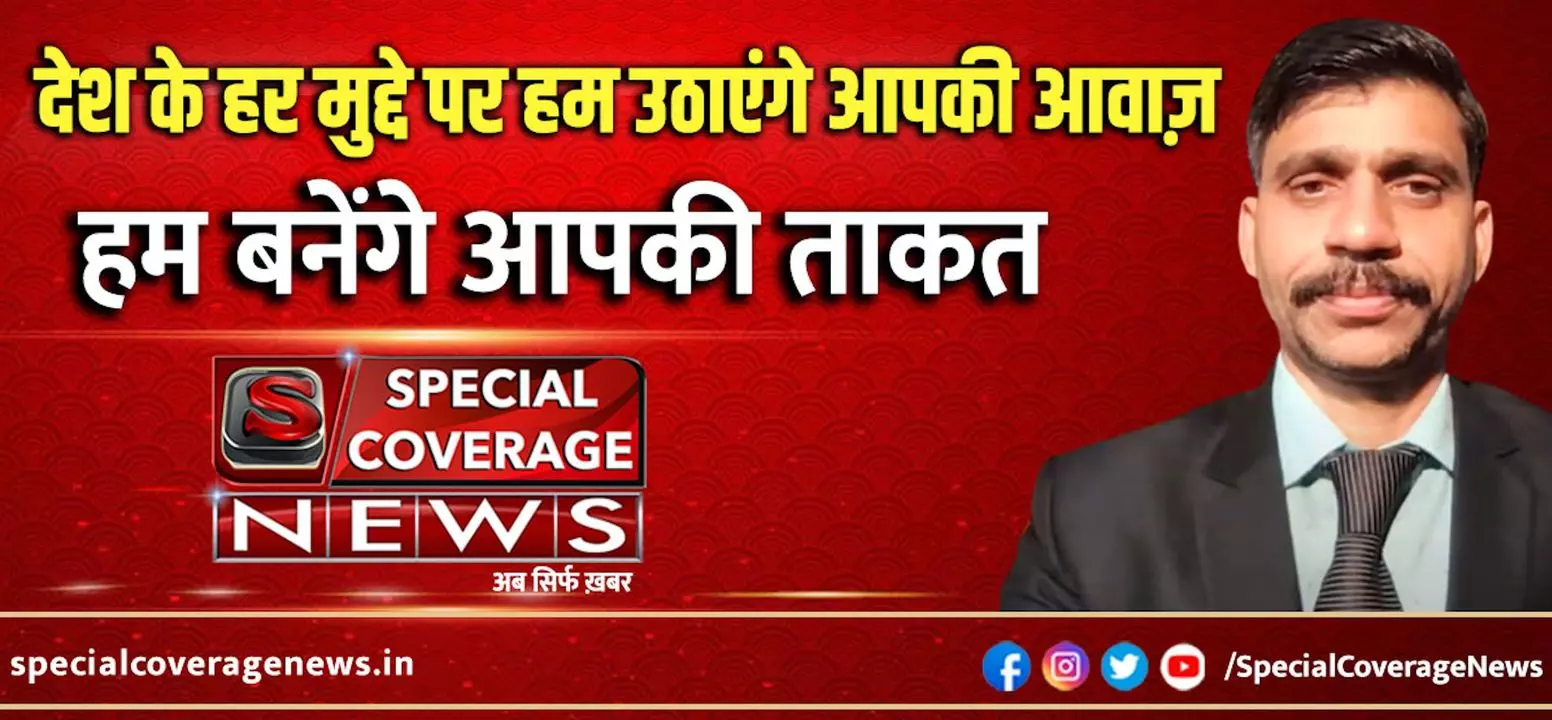- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- लखनऊ
- /
- आंबेडकर-लोहिया के नाम...
आंबेडकर-लोहिया के नाम भुना चुके लोग अब परशुराम को लेकर बाजार में उतरे

जितेंद्र कुमार
देश की राजनीति जिस मोड़ पर है वहां किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कोई भी कार्रवाई अब उतना नहीं चौंकाती, जितना कि पहले चौंकाती थी. अभी तीन-चार दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एकाएक घोषणा की कि उनकी पार्टी हर जिले में 'भगवान' परशुराम की 108 फुट की प्रतिमा लगवाएगी. अब उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का समय बसपा का था. बसपा ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में लौटेगी तो न केवल परशुरामजी की बड़ी प्रतिमा लगवाएगी बल्कि परशुरामजी के नाम का अस्पताल भी बनवाएगी.
जो लोग भी सामाजिक-आर्थिक वैचारिकी को समझते हैं, वे बसपा-सपा के बदले रुख़ से हतप्रभ हो रहे हैं. वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आंबेडकर, कांशीराम और लोहिया की वैचारिक विरासत के लोग किस आधार पर परशुराम के नाम पर हर जिले में आदमकद प्रतिमा और अस्पताल खोलने की बात कर रहे हैं. वे यह भी नहीं सोच पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के दो बड़े राजनीतिक दलों के इस पतन का क्या कारण हो सकता है.लोग तो बस इनके अतीत की राजनीतिक विरासत को याद करके हतप्रभ हैं.
यहां सवाल यह नहीं है कि परशुराम की प्रतिमा लगनी चाहिए अथवा नहीं. यहां सवाल सिर्फ यह है कि सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों राजनीतिक दलों में जिस परशुराम की प्रतिमा लगाने की होड़ मची है उसे लोग किस रूप में जानते हैं और उनकी सामाजिक विरासत क्या है?
परशुराम एक मिथकीय चरित्र है जिसका राम की तरह कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है. फिर भी आस्था से ही हमारा देश चल रहा है जहां वैज्ञानिक सोच की अब न जरूरत रह गयी है और न ही गुंजाइश बची है. इसलिए मिथकीय चरित्रों पर राजनीति भी हो रही है और उसी के आधार पर एजेंडा भी सेट हो रहा है. फिर भी यह तो जानना ही चाहिए कि आखिर जिस 'भगवान' परशुराम के लिए बसपा और सपा ने अपने कोर वोट को दांव पर लगा दिया है उसका इतिहास क्या है और हम उन्हें किस रूप में जानते हैं.
बचपन से हमें परशुराम के बारे में जो सुनने को मिला है उसके अनुसार वे काफी गुस्सैल किस्म के आदमी थे और अपने विरोधियों का सिर हाथ में रख कर फरसे से तत्काल कलम कर देते थे! बहुत बाद में पता चला कि वे इतने आज्ञाकारी बेटा थे कि अपने पिता के कहने पर उन्होंने अपनी मां का गला फरसा से काट दिया था. अगर इसे हिन्दुत्व के एजेंडा के अगल-बगल में रखकर देखें तो मामला काफी दिलचस्प दिखता है. कोई भी बेटा अपनी मां की हत्या करके कैसे आदर्श पुरुष बन सकता है.लेकिन हिन्दुत्व के एजेंडा के अनुसार वह हिन्दू श्रेष्ठ हिन्दू है जो पितृसत्ता को बनाये रखने में मददगार साबित हो. यहां परशुराम हिन्दुत्व के एजेंडा में बेहतर व प्रतापी बेटा बनकर निकलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी मां का गला काट दिया था.
यह है सपा-बसपा के आधुनिक नायक की कहानी. लेकिन सवाल यह भी है कि सपा-बसपा तो राजनीतिक रूप से पितृसत्ता का समर्थन नहीं करती हैं, फिर सवर्ण व पितृसत्ता के इतने बड़े पोषक व गुस्सैल परशुराम की प्रतिमा हर जिले में क्यों लगवाना चाह रहे हैं? यही वह रहस्य है जिसे समझने की जरूरत है.
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद धीरे-धीरे ब्राह्मणों का बीजेपी से मोहभंग होना शुरू हुआ है. कई राजनीतिक व सामाजिक कारण रहे हैं, लेकिन विकास दूबे की फर्जी हत्या के बाद ब्राह्मणों में यह संदेश गया कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है. विकास दूबे के आपराधिक रिकॉर्ड को देखा जाय तो हम पाते हैं कि जितने अपराध या हत्याएं विकास ने की थीं, उसमें से अधिकांश हत्या या अपराध ब्राह्मणों के साथ हुए. उधर बीजेपी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का शिलान्यास करवा दिया और सपा-बसपा मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर हिन्दुत्व के पक्ष में चुप्पी साधे रहे. इसी बीच 4 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियांका गांधी वाड्रा ने सॉफ्ट हिन्दुत्व की लाइन ले ली. वैसी परिस्थिति में सपा-बसपा को लगा कि अगर ब्राह्मणों के दस फीसदी वोट बीजेपी छोड़कर बाहर जाते हैं तो किधर जाएंगे?
लगभग 25 वर्षों के बारी-बारी से सपा-बसपा के शासनकाल में दोनों दलों ने देखा है कि ब्राह्मण की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है. निजी तौर पर बाद में मुलायम सिंह कहते भी रहे हैं कि ब्राह्मण को किनारे करके हम सत्ता से पार नहीं पा सकते जबकि मायावती को तीन बार मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के सहयोग से ही मिली थी. अंतिम बार जब वह पूर्ण बहुमत से सत्ता में आयीं तो उस समय ब्राह्मणों ने उन्हें काफी वोट भी दिया था. लेकिन याद रखिए, वे दोनों ही नेता सत्ता में आये तो जरूर लेकिन अपनी विरासत के साथ विश्वासधात करके सत्तासीन हुए.
वैसे एक सवाल लाजिमी है कि अंबेडकर और लोहिया की विरासत की बात करने वालों को ब्राह्मणों की याद इतनी शिद्दत से क्यों आने लगी है?
इसका जवाब इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी राजनीतिक टिप्पणीकार इस बात को बोलने से कतराते हैं. पूरे देश में दलितों की राजनीति का एकमात्र प्रवक्ता (राजनीति की बात हो रही है) मायावती रही हैं. वह जब ब्राह्मणों को अपने फोल्ड में लाने की बात करती हैं तो दलित बुद्धिजीवियों में काफी तीक्ष्ण प्रतिक्रिया होती है. दलित बुद्धिजीवी मानते हैं कि उनके पिछड़ेपन में ब्राह्मणों की भूमिका सबसे विध्वंसकारी रही है. इसलिए मायावती के इस तरह के समीकरण पर सबसे उग्र प्रतिक्रिया दलित कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती है.
यही बात अखिलेश यादव के साथ नहीं है. इसका कारण यह है कि मंडल की राजनीति के बाद पिछड़ों के कुछ खास तबकों में राजनीतिक चेतना आयी है जिसका सबसे अधिक असर उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखता है. दुखद यह है कि अखिलेश यादव अगर मायावती की तरह ही कोई प्रतिक्रियावादी बात बोलते हैं तो पिछड़ी जाति की बौद्धिक जमात (खासकर यादव) इस मामले पर चुप्पी साध लेती है.
मंडल के बाद राजनीति में जितनी तेजी से बदलाव आया उस बदलाव के अनुरूप दोनों पार्टियां चल नहीं पायीं. पिछले 25 वर्षों का शासनकाल उत्तर प्रदेश के दलितों और पिछड़ों के लिए कब्रगाह जैसा रहा है. भाजपा और कांग्रेस सत्ता के लिए ही सही, दिखावा ही करती रहीं, लेकिन जब से सपा-बसपा सत्ता में आयी हैं इन्होंने उन सभी चीजों को उसी तरह नष्ट किया जिस रूप में पहले कांग्रेस कर रही थी और बाद में भाजपा करने लगी.
इन दोनों दलों ने अपने शासनकाल में स्कूलों, कॉलेजों और हस्पतालों को तहस नहस कर दिया. ये वे संस्थान थे जिन्हें बचाये जाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी. दलित-बहुजन नेतृत्व इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया कि इन संस्थानों को बेहतर करके ही वो अपने आधार वोटर-समर्थक को मजबूत कर सकते थे. उल्टे उसने भी इन्हें बाजार के भरोसे छोड़ दिया. अगर पिछले पांच-छह वर्षों के इतिहास को देखें तो हम पाते हैं कि वही लोग बीजेपी के खिलाफ मोर्चे पर हैं जिनकी शिक्षा-दीक्षा सरकारी स्कूलों में हुई है. वे सब के सब सरकारी स्कूलों के पढ़े-लिखे हैं. मुलायम, मायावती और अखिलेश ने उन सभी स्कूलों कॉलेजों को नष्ट होने दिया. आज वास्तविकता यह है कि सरकारी स्कूल वैसी स्थिति में ही नहीं रह गई है जहां दलितों-पिछड़ों के बच्चे जाकर शिक्षा हासिल कर कुछ बनने का सपना देख सकें.
सूचना के तंत्र पर सवर्णों का पूरा कब्जा है. वहीं से माहौल बनता है और वहीं से नेताओं की छवि चमकायी और मलिन की जाती है. 25 वर्षों के शासनकाल में इन नेताओं ने एक भी ऐसा तंत्र विकसित नहीं किया जहां से वे अपने समर्थकों तक अपनी बात पहुंचा सकें. सत्ता में इतने दिनों तक रहने के बाद उन्हें विश्वास हो गया है कि अगर फिर से सत्ता में वापस आना है तो ब्राह्मणों के समर्थन के बिना वापसी नामुमकिन है क्योंकि सूचना तंत्र पर सवर्णों का एकछत्र राज है.
जब वे सत्ता में रहे तो आरक्षण को लागू करने का काम नौकरशाहों पर छोड़ दिया गया जो खुद आरक्षण विरोधी थे. नौकरशाही ने पूरी कोशिश की कि आरक्षण कम से कम लागू हो, परिणाम यह हुआ कि तंत्र चलाने के लिए उनके लोग ही नहीं तैयार हो पाये.
बची-खुची उम्मीद इन दलित-पिछड़े नेताओं के आर्थिक भ्रष्टाचार और परिवारप्रेम ने लील ली. ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टियां कम भ्रष्ट हैं. उन दोनों पार्टियों ने अपने लिए एक समानांतर तंत्र खड़ा कर लिया है जो हर जरूरत में उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन इन दोनों दलों ने कभी वैकल्पिक मॉडल के बारे में सोचा ही नहीं.
चूंकि मायावती व अखिलेश जानते हैं कि बिना ब्राह्मण के फिर से सत्ता पाना असंभव है इसलिए परशुराम के सहारे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं. इस चक्कर में वे दलित-पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की परवाह भी नहीं कर रहे जो इनके साथ चट्टान की तरह 25 वर्षों से लगातार खड़े रहे हैं.