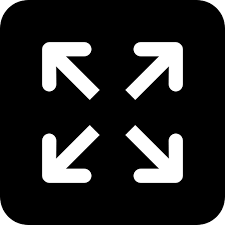- प्रो. दिग्विजय नाथ झा-
''चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझपर बेवफाई का।
मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे इस चमन की रहनुमाई का।''
सचमुच कितनी बड़ी विडंबना है कि चरम चुनावी सफलता एवं अतिलोकप्रियता के बाद भी श्रद्धेय नरेन्द्र दामोदरदास मोदी मौजूदा आर्थिक हालात की विद्रूप हकीकत को स्वीकार करने की हिम्मत आज की तारीख तक नहीं जुटा पा रहे हैं, बावजूद इसके कि थॉमस पिकेटी, इमैनुएल सैज एवं गेब्रियल जुकमैन सरीखे विश्वस्तरीयमशहूर अर्थशास्त्री की वर्ल्ड इनइक्विलिटी रिपोर्ट चीख-चीख कर बयां कर रही है कि आय असमानता में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल रहा है। निम्न मध्यम वर्ग के पचास फीसदी व्यस्क भारतीयों की सालाना कमाई जहां सिर्फ 53 हजार रूपए के आसपास है, वहीं केवल एक फीसदी भारतीयों के अधीन भारत की 33 फीसदी सम्पत्ति है और इससे भी अधिक शर्मनाक तो यह कि तकरीबन 80 करोड़ भारतीयों के लिए प्रतिमाह पांच किलो मुफ्त अनाज की उपलब्धता को ही भारत के मौजूदा यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी करार देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं।
कोविड महामारी के प्रकोप से भारत अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। दैनिक मजदूरी से गुजारा करनेवाली जनता दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भारत में अब भी जद्दोजेहद करती नजर आ रही है, पर भारतीय धन-कुबेरों के खजाने में धन की बेतहाशा हो रही बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोविड की पहली लहर के दौरान भारत के शीर्ष सौ अरबपतियों की कुल सम्पत्ति में नकारात्मक जीडीपी के बावजूद 12.98 लाख करोड़ रूपए का इजाफा हुआ और दूसरी लहर के दौरान 17.22 लाख करोड़ रूपए की बृ़द्धि हुई, जबकि कोविड की पहली और दूसरी लहर की भयावहता का नतीजा यह हुआ कि प्रतिदिन 150 रूपए से कम कमाई करनेवाले भारतीयों की तादाद तकरीबन छह करोड़ बढ़ गई, जिससे कि वर्ष 2021 के दिसम्बर महीने तक प्रतिदिन 150 रूपए से कम कमाई करनेवाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 13 करोड़ 40 लाख के आसपास पहुंच गई।
कोविड की पहली व दूसरी लहर के दौरान बीते डेढ़ सालों में लगभग डेढ़ करोड़ भारतीयों ने अपनी नौकरी गंवायी। भारत में लेबर पार्टीसिपेशन दर 40 से नीचे चली गई यानी कि करोड़ों लोग रोजगार बाजार से बाहर हो गए। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दस्तक देने से चंद दिनों पूर्व ही वर्ल्ड इनइक्विलिटी रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि भारत की कार्पोरेट और हाउसहोल्ड अर्थव्यवस्था एक-दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है और स्थिति इस कदर दयनीय है कि वर्ष 1974 के बाद भारत फिर से मास पोवर्टी वाला देश बन गया है।
भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री संभवतः इससे बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं होंगे कि प्रतिव्यक्ति औसतन 1165520 रूपए की सलाना कमाई करनेवाले व्यस्कों की तादाद देश में इन दिनों एक करोड़ 30 लाख के आसपास है, जबकि प्रतिव्यक्ति औसतन 9230 रूपए की मासिक कमाई करनेवाले व्यस्कों की संख्या भारत में लगभग 65 करोड़ है और चिंताजनक तो यह कि नोटबंदी के बाद से ही भारतीय व्यस्कों के वेतन मजदूरी में बढ़ोतरी लगातार महंगाई से पिछड़ती रही है, बावजूद इसके कि कोविड की पहली व दूसरी लहर के दौरान बीते डेढ़ सालों में स्वास्थ्य मद में 66 हजार करोड़ रूपए भारतीयों ने नियमित खर्च के अतिरिक्त व्यय किए और हद तो यह कि वर्ष 2014 से पूर्व तक केन्द्र सरकार के प्रति सौ रूपए के राजस्व में देश के टॉप 10 फीसदी अमीरों से 40 रूपए तथा आमलोगों से 60 रूपए आते थे, परंतु आज की तारीख में केन्द्र सरकार के प्रति सौ रूपए के राजस्व में देश के टॉप 10 फीसदी अमीरों से 25 रूपए एवं आमलोगों से 75 रूपए आ रहे हैं।
ताज्जुब की बात तो यह कि वस्तु एवं सेवा कर प्रावधानों के लागू होने के बाद भी बीते पांच सालों में पेट्रो उत्पादों से टैक्स संग्रह 700 फीसदी बढ़ा है। सच पूछिए तो कोविड की पहली एवं दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय आय का 80 फीसदी नुकसान आम भारतीयों के खाते में गया, जबकि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व यूरोप में सरकारों ने नगदी मदद के जरिए अपने कामगारों की कमाई में कमी नहीं होने दी। बेरोजगारी की छाया में महंगाई का नया संस्कार आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं ही नहीं भारतीयों की आर्थिक समझ भी बदल दी है। अर्थव्यवस्था में कामकाज शुरू होने और रिकवरी के ढोलवादन के बावजूद श्रम बाजार की हालत बदतर बनी हुई है।
मनरेगा में काम मांगनेवालों में युवाओं की तादाद आठ साल के सबसे ऊँचे स्तर पर है। मनरेगा के मजदूरों में करीब 12 फीसदी श्रमिक 18 से 30 साल की आयुवर्ग के हैं। वर्ष 2019 में यह प्रतिशत 7.3 था। सर्वाधिक दुःखद तो यह कि मनरेगा जो कभी गांव में प्रौढ़ आबादी के लिए मौसमी मजदूरी का जरिया थी, वह इन दिनों 18 से 30 साल की आयुवर्ग के भारतीयों की आखिरी उम्मीद बन गई है। बेकारी से बढ़ रही गरीबी वित्तीय विसंगतियों का हिस्सा है, लेकिन सरकारें गरीबी की बहुआयामी नापजोख के तरीके बदल रही है और ऐसा इसलिए कि सरकारें आमतौर पर गरीबी छिपाती है। बहरहाल, कोविड की पहली एवं दूसरी लहर के बाद से ही भारत में गरीबी को केवल कमाई के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास के 12 पैमानों पर मापने की जद्दोजदह जारी है। इसमें पोषण, बाल मृत्यु दर; गर्भवती माताओं की देखभाल, स्कूली शिक्षा, स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, घरेलू गैस सिलेंडर, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली, पक्का आवास, मोबाइल फोन एवं बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाते की उपलब्धता को शामिल किया गया है। इस नापजोख की स्याह हकीकत यह है कि बैंक के व्यस्क खाताधारकों एवं मोबाइल फोन रखनेवाले भारतीयों को गरीब नहीं माना गया है, तभी तो दिल्ली में गरीबी पांच फीसदी से कम बताई गई है और हद तो यह कि इस आधुनिक पैमाइश से भी जो निष्कर्ष निकलते हैं वे भी कोई तमगे नहीं हैं जिनपर गर्व किया जाए।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हालिया रिपोर्ट चीख-चीख कर बयां कर रही है कि विकास के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करनेवाले चंद भारतीय राज्यों में से कोई एक भी विकसित देश जैसा नहीं है। धीमी पड़ती विकास दर, बढ़ते बजट घाटों, बेसिर पैर की महंगाई और ढांचागत चुनौतियों की रोशनी में यह पैमाइश हमें साफ-साफ बता रही है कि बीते दो दशकों में भारत की औसत विकास दर छह फीसदी रही, जो इससे पहले के तीन दशकों के करीब दोगुनी है, पर बीते बीस सालों में सबसे अगड़े तथा पिछड़े भारतीय राज्यों में आय असामनता लगभग 337 फीसदी बढ़ गई यानी कि उत्तर प्रदेश व बिहार आय के मामले में कभी भी सिक्किम या पंजाब नहीं हो सकेगा तथा बिहार व यूपी के लोग जन्मस्थान दुर्भाग्य का चिरंतन सामना करेंगे। यद्यपि, भारत में राजनीतिक खांचे इतने वीभत्स हो चुके हैं कि विकास में जन्मस्थान की भूमिका पर निष्पक्षशोध दुर्लभ हैं, अलबत्ता इस सफेद सच की वजहें तलाशी जा सकती है। विश्व बैंक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2020 के अपने अध्ययन में पाया कि दुनिया में आर्थिक सुधारों का पूरा फार्मूला केवल तीन उपायों में सिमट गया है। प्रथम है निजीकरण, द्वितीय नियमों-कानूनों का उदारीकरण और तृतीय सब्सिडी समाप्तिकरण।
दुनिया के अर्थविद इसे हर मर्ज की संजीवनी समझ कर चाटते हैं। मानो कि आर्थिक सुधारों का मतलब सिर्फ इतना ही हो। ताज्जुब है कि राजनीति लोगों की नब्ज क्यों नहीं समझ पाती ? अर्थविद अपने सिद्धांत कोटरों से बाहर क्यों नहीं निकल पाते ? सुधार उन्हीं को क्यों डराते हैं जिनको इनका फायदा मिलना चाहिए ? जबाव के लिए असंगति की इस गुफा में गहरे पैठना जरूरी है। सुधारों की परिभाषा केवल जिद्द तक सीमित ही नहीं हो गई है बल्कि इनके केन्द्र में आमलोग नजर नहीं आते। भले ही आर्थिक सुधार के सरकार के फैसले बाद में बड़ी आबादी को फायदा पहुंचायें, लेकिन इनके आयोजन एवं संवादों के मंच पर कॉर्पोरेट घरानों के एकाधिकार दिखते हैं जैसे कि बैंकों के निजीकरण की चर्चाओं के केन्द्र में जमाकर्त्ताओं के हित को तलाशना मुश्किल है। कृषि सुधारों का आशय तो कृषकों की आय बढ़ाना था, परंतु उपायों के पर्चे पर कॉर्पोरेट घरानों के चित्र छपे थे, इसलिए सुधार जिनके लिए बनाए गए थे वही लोग बागी हो गए।
कृषि भारत की सबसे पुरानी आर्थिक गतिविधि है। सदियों से लोकमानस में यह सम्पत्ति के मूलभूत अधिकार और अजीविका के अंतिम आयोजन के तौर पर उपस्थित है। उद्योग, सेवा या तकनीक जैसे किसी दूसरे आर्थिक उत्पादन की तुलना में खेती बेहद व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक आर्थिक उपार्जन है। कृषि सुधारों का सबसे सफल आयोजन चीन में सिर्फ व सिर्फ इसलिए संभव हुआ कि देंग शियाओपिंग ने 1981 में कृषि के उत्पादन व लाभ पर किसानों का एकाधिकार सुनिश्चित कर दिया। आर्थिक सुधार पहले चरण में बहुत सारी नेमतें बख्शते हैं।
जैसे कि डा0 मनमोहन सिंह के 1991 के आर्थिक सुधार से भारत को बहुत कुछ मिला। लेकिन प्रत्येक सुधार 1991 वाला नहीं हो सकता है। आर्थिक सुधार दूसरे चरण में कुर्बानियां मांगते हैं। इसके लिए सुधारों के विजेताओं के ईमानदार मुल्यांकन चाहिए। अर्थशास्त्री मार्केट सक्सेस की दुहाई देते हैं, मगर मार्केट फेल्योर पर कतई भी चर्चा नहीं करते, जिसके कि गहरे तजुर्बे आम लोगों के पास हैं। इसलिए सरकारी नीतियों के अर्थशास्त्र पर आमलोगों का अनुभवजन्य अर्थशास्त्र भारी पड़ने लगा है। सुधारों से चिढ़ बढ़ रही है, क्योंकि सरकारें इनपर बहस सिद्ध सहमति नहीं बनाना चाहती।
जीएसटी हो या कृषि बिल सरकार ने उनके सवाल ही नहीं सुने जिनके लिए इनका अवतार हुआ था। सनद रहे कि लोगों को सवाल पूछने की ताकत देने की जिम्मेदारी भी सत्ता की है। शासन को ही यह तय करना होता है कि ताकत का केन्द्रीकरण किस सीमा तक किया जाए और फैसलों में लोगों की भागीदारी किस तरह सुनिश्चित की जाए। इससे कतई भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि बीते ढाई दशकों में लोगों में आर्थिक सुधारों के फायदों और नुकसानों की समझ बनी है। मंदी से टूटे लोग कमाई और जीवन स्तर में ठोस बेहतरी के प्रमाण व उपाय चाहते हैं। यही वजह है कि विराट प्रचारतंत्र के बावजूद सरकार लोगों को सुधारों के फायदे नहीं समझा पाती तथा 80 करोड़ भारतीयों के लिए प्रतिमाह पांच किलो मुफ्त अनाज की उपलब्धता एवं साढ़े तीन करोड़ किसानों को दी जा रही प्रतिमाह पांच सौ रूपए की सहायता को ही बड़ी कामयाबी बताती।
सुधारों की भाषा उनके लिए ही अबूझ हो गई जिनके लिए उन्हें गढ़ा जा रहा है। सरकारें और उनके अर्थशास्त्री जिन्हें सुधार बताते हैं जनता उन्हें अब सत्ता काअहंकार अथवा कि पाखंड समझने लगी है। कृषि कानूनों की दंभजन्य घोषणा पर जितनी चिंता थी उतनी ही फिक्र इनकी वापसी पर भी होनी चाहिए जो सरकारों से विश्वास टूटने के प्रमाण का विस्तार है। मसलन, ऐसा कहां होता होगा कि भारतीय बैंक 2016 से जिन राजनैतिक लोगों को खाता खोलने और सेवाएं देने के लिए भी किस्म-किस्म की पड़ताल कर रहे हैं उन्हीं लोगों को सरकार कोऑपरेटिव बैंकों में डायरेक्टर बनाती रही। शायद पाखंड ही भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत अदृश्य बहुदलीय शपथ है। 2021 का घटनाक्रम अबतक का सबसे नायाब नमूना है।
2021 के जून के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों में निदेशक व प्रबंध निदेशकों के पद पर सांसदों, विधायकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के मनोनयन पर रोक लगा दी। इस तरह का कोई आदेश पहली बार जारी हुआ था। अलबता इस आदेश की पावती जबतक रिजर्व बैंक को मिलती तबतक केन्द्र सरकार में नया सहाकरिता मंत्रालय बनाने की फाइल चल चुकी थी। यानी कि घोटालों एवं राजनीतिक दखल खत्म करने की कोशिश हुई तो सरकार के दूसरे हाथ ने सियासी दखल की संभावनाओं को ही संस्थागत बना दिया। बहस तो सहकारिता को साफ-सुथरा, स्वायत और पेशेवर बनाने की थी। लेकिन मंत्रालय के जन्म की बधाई बजते ही सहकारी राजनीति के सहारे देश की राजनीति पर पकड़ मजबूत करने के 'गेम चेंजर प्लान'के नए डिजाइन पर तालियां बज उठी।